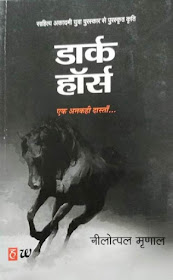हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ चन्द्रशेखर आज़ाद का आज जन्मदिवस है. पंडित जी के सपनों का समाजवादी भारत था, जिसमें सभी को रोटी, कपड़ा, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार का प्रबंध होना था. आज़ाद को याद करते हुए उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के संस्मरणों का एक आलेख पढ़ें
मैं तो एक मुश्ते गुबार हूं...
बटुकेश्वर दत्तसरदार की गुनगुनाहट आज भी मेरे कानों से टकरा रही है- मैं तो एक मुश्ते-गुबार हूं... धोकर निचोड़े गए कपड़ों को झटके दे-देकर जैसे वह धूप में फैला रहा हो और पूरी तन्मयता के साथ गुनगुना रहा हो. कानपुर स्थित सुरेश दादा के मेस की दूसरी मंजिल की छत पर किशोर सरदार के कपड़े धोने का दृश्य अब भी उसी तरह अम्लान है-कंधे सहित सिर पर लिपटा केश-गुच्छ, कमर में एक कच्छा छोड़कर पूरा नंगा बदन, जल की धार पर वह लगातार कपड़े पटक रहा है. साबुन के शुभ्र फेन उड़-उड़कर इधर-उधर फैल रहे हैं. मैं बगल में बैठा अन्य कपड़ों पर साबुन घिस रहा हूं और सरदार बार-बार वही एक पंक्ति दुहराये जा रहा है- मैं तो...
सन् उन्नीस सौ चौबीस के शुरू का कोई महीना. मैं उन दिनों कानपुर के बंगाली मिडिल स्कूल का विद्यार्थी और पारिवारिक अनुशासन की आंखें बचाकर क्रांतिकारी दल की शाखा का एक सक्रिय कार्यकर्त्ता. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र 'प्रताप' से सम्बध्द, दल के प्रमुख नेता श्री सुरेशचंद्र के निर्देशानुसार एक शाम उनसे मिलने कम्पनी बाग गया. क्यों और किसलिए बुलाया गया था, यह पूछना दलीय अनुशासन के विरुध्द था और आदेश पर आंख मूंदकर चलना ही हमारे विप्लवी जीवन का प्रथम पाठ. इसलिए हर तरह की परिस्थिति के प्रति अपने को तैयार कर समय से वहां पहुंचा. सुरेश दादा नहीं थे. बाग के एक छोर से दूसरे तक मेरी चंचल निगाहें ढूंढ़ गयीं, पर कहीं पर भी वह नजर नहीं आया. मुझे आश्चर्य हुआ क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में इस तरह की भूल पहले कभी देखने को नहीं मिली थी. घनघोर अंधेरी रात में भी मूसलाधार वर्षा सिर पर झेलते हुए, सीआईडी की निगाहें बचाता निर्दिष्ट कार्य के लिए ठीक जगह निर्धारित समय पर हाजिरी बजाने में इसके पहले मुझसे कभी भूल नहीं हुई थी. फिर आज प्रमुख क्रांतिकारी नेता के निर्देश और कार्य में यह अंतर क्यों?
इसी उधेड़बुन में पड़ा था कि मेरी आंखें एक घनी, कांटेदार झाड़ी से जाकर उलझ गयीं. क्या ही अजीब, रोंगटे खड़े कर देने के साथ-साथ हंसाने वाला दृश्य! झाड़ी केऊपर एक सफेद पगड़ी का सिरा लगातार दायें से बायें और बायें से दायें मोर की पखी की तरह डोल रहा था. मैं नजर गड़ाये उसे देखता रहा. बीच-बीच में वह स्थिर हो जाता और फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह अपनी चाल पकड़ लेता. बाग के निस्तब्ध वातावरण में, जबकि संध्या का रक्तिम प्रकाश रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाने की तैयारी कर रहा हो, कांटेदार झाड़ी के ऊपर से सफेद पगड़ी का वह हिलता सिरा इशारे से जैसे मुझे अपने पास बुला रहा था. मैं आगे बढ़ा. झाड़ी के समीप पहुंचते ही उस सफेद पगड़ी का अधिकारी साढ़े पांच फुट से भी लंबा एक सिख युवक मेरी आहट पर उछलकर खड़ा हो गया. उसकी काली चमकती आंखों में शंका की भावना और लम्बी लटकती दोनों भुजाओं पर कमीज के चढ़े आस्तीन, दृढ़ मुट्ठियों में बंद लंबी उंगलियां, दोनों गालों पर दाढ़ी की हल्की रेखा, सिर पर पगड़ी में कैद केश-गुच्छ, जिसकी कुछ लटें बाहर झूल रहीं थीं.
मेरे सामने वह सिख युवक चैलेंज का भाव चेहरे पर लिए खड़ा था और मैं उसकी तात्कालिक मुद्रा के प्रति उदासीन, कि तभी बगल में निश्चल गिरिराज की भांति बैठे विप्लवी सुरेश दादा पर ध्यान गया. मुझे देखकर उनके चेहरे पर चिर-परिचित मुस्कराहट खेल गयी और सरदार शांत पड़ा. उसकी दृढ़ मुट्ठियों की उंगलियां सहज और शिथिल हुई. मुझ नवागंतुक को देखते ही जो चमक और खून उसकी आंखों में उतर आया था, सुरेश दादा की मुस्कराहट से जैसे पूरे चेहरे पर लालिमा बन फैल गया और मुझे लगा अपनी अनावश्यक दृढ़ता के लिए वह कुछ झेप-सा रहा है. सुरेश दादा ने हंसते हुए हम दोनों को आमने-सामने बैठाया और उस तरुण सरदार से मेरा परिचय कराया नाम- बलवंत सिंह पंजाब के नेशलनल कालेज में बीए के छात्र हैं.
प्रमुख क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस निकटतम सहयोगी शचींद्रनाथ सान्याल 'बंदी जीवन' के लेखक एवं बाद में काकौरी षड़यंत्रा के प्रमुख अभियुक्त उस समय उत्तरी भारत में क्रांतिकारी दल के प्रमुख संगठनकर्त्ता थे. पंजाब नेशनल कालेज के अध्यापक श्री जयचंद्र विद्यालंकार की मार्फत शचींद्र दादा से उस सिख नवयुवक का परिचय हुआ और वह क्रमश:विप्लवी संगठन में खिंच आया. उसकी क्रांतिकारी विचारधारा देखते हुए परिवार के लोग छात्रावस्था में ही उसका विवाह कर देने का निर्णय कर चुके थे, लेकिन क्रांतिपथ के पथिक उस तरुण को अपने विवाह का प्रस्ताव मंजूर नहीं था और उसी से मुक्ति पाने के लिए तमाम पारिवारिक आत्मीयता एवं परिवार के लोगों से संबंध-विच्छेद कर वह लाहौर से सुरेश दादा के आश्रय में कानपुर भाग आया था.
रूसी विप्लवियों का प्रभाव उसकी स्मृतियों में था और उन्हीं की तरह उसने भी शपथ ले रखी थी कि जीवन में न किसी से प्रेम करेगा, न किसी का प्रेम-पात्र बनेगा, न विवाह करेगा, न किसी का विवाह रचायेगा. उससे संबंधित ये तमाम बातें मुझे धीरे-धीरे बाद में मालूम हुईं जब अपने पहले परिचय के बाद प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी हम एक-दूसरे के करीब आते गए. और उसी वर्ष यानी 1924 में ही! जीवनदायनी गंगा का प्रलयंकारी प्लावन! दोनों तटों पर बसे कानपुर शहर के साथ-साथ अनगिनत गांव उस प्लावन के शिकार हुए थे. प्लावन के शिकार ग्रामवासियों ने वृक्ष की ऊंची डाल पर आश्रय लिया. बहते हुए लोगों को सहारा देने के लिए गंगा पुल पर मोटी-मोटी रस्सियां बांधकर लटकायी गयीं थीं, ताकि धारा के साथ बहते हुए लोग उन रस्सियों को पकड़कर अपने प्राण बचा सकें.
शहर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कैम्प डाले गएं. 'तरुण संघ' नाम की एक संस्था काम कर रही थी और हमें भी सेवा दल में काम करने की पुकार मिली. बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों की सेवा में मैं जुट गया. बलवंत सिंह साथ था. घर के अनुशासन की उपेक्षा कर किसी सार्वजनिक सेवा कार्य के लिए घर छोड़ दिन-रात काम करने का मेरा वह पहला मौका था. बलवंत का नाता घर से पहले ही टूट चुका था, इसलिए उसे किसी तरह के पारिवारिक अनुशासन की चिंता थी नहीं. सेवा कार्य में जुट जाना उसके लिए अनायास था जबकि उसी काम के लिए मेरे किशोर मन ने घर के विरुध्द पहली दफा विद्रोह का रास्ता अपनाया.
हम दोनों की डयूटी प्राय: एक साथ ही पड़ती. रात में हम दोनों गंगा के अंधेरे तट पर खड़े होकर हाथों में जलती लालटेन लिए शून्य में अविराम हिलाया करते ताकि प्लावन की तीक्ष्ण धारा में बहते हुए मनुष्य-मवेशी अंधेरी रात में किनारे का संकेत पा सकें और जब कभी मवेशियों का कोई झुंड उस रोशनी के सहारे हमारे पैरों के पास पहुंच जाता, हम उसे बाहर निकालते, फिर उसे रखने की व्यवस्था की जाती थी. दिन के समय हम दोनों मल्लाहों के साथ निकलते और बाढ़ग्रस्त निराश्रित परिवारों को उनकी बची हुई सामग्री के साथ नाव पर लादकर गंगा तट के कैम्पों में पहुंचाते किशोर सरदार का हृदय यह सब देख-देखकर पसीजता रहता और उसकी आंखों में उस वक्त एक अव्यक्त-सी करुणा समायी होती थी. शहर के पास ही कल्याणपुर के बाढ़ पीड़ित कैम्प का वह दृश्य आज भी मेरी आंखो में सुरक्षित है.
बाढ़ की प्रलंयकारी लीला में सबकुछ गंवा कर हताश, भूखे-असहाय लोगों का वह हुजूम! उनकी हृदय वेधी चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा था. भोजन की प्रतीक्षा करते स्त्री-पुरुष अलग-अलग कतारों में पत्तल के सामने बैठे थे कि तभी गर्म पूड़ियों की टोकरी दोनों हाथों से ऊपर उठाये तरुण सरदार दिखाई पड़ा. सिर पर सफेद रेशमी पगड़ी, बदन में साधारण कपड़े की कमीज जिसकी दोनों आस्तीनें ऊपर चढ़ी थीं. मुझसे आंखें मिलते ही उसके होठों पर स्वत: स्फूर्त मुस्कान एवं आंखों में चमक कौंध उठी, लेकिन बातचीत का समय कहां.वह उत्साह एवं उमंग के साथ भूख से बेचैन लोगों की कतार की तरफ बढ़ गया.
बाढ़ पीड़ितों की सहायता-सेवा के उस दौर ने हम दोनों को एक-दूसरे के करीब लाने में काफी मदद की. उस दिन क्षुधित, सर्वहारा जनों के बीच पूड़ियां बांटने का सरदार का अंदाज, काम के प्रति उसकी लगन एवं निष्ठा आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं. पूड़ियां परोसने वाले उसके हाथों ने बाद के क्रांतिकारी जीवन में उसी निष्ठा के साथ पिस्तौल या बम भी चलाये. उस रोज किसे मालुम था कि परवर्ती क्रांतिकारी जीवन में हमें अति साधारण भोजन भी नियमित रूप से नसीब न होगा या यह कि पूड़ियां परोसने वाले उन हाथों पर सूखी रोटी और नमक ही शेष जीवन के आधार होगें.
उन दिनों हम दोनों के किशोर जीवन में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण भाव के साथ-साथ जो सबसे बड़ा आकर्षण था, वह शहर (कानपुर) के पास कनालफाल के समीप गंगा के तट पर बैठ उसकी सुषमा को अनवरत निरखते रहना और बीच-बीच में किसी विषय, किसी बात या योजना पर परस्पर विचार-विमर्श करना. इसी सिलसिले में अकसर हम क्रांतिकारी जीवन के आने वाले दिनों की कल्पना में तल्लीन हो जाया करते. प्रसिध्द क्रांतिकारी जीवनियों या क्रांति से संबंधित साहित्य का पाठ हम यहीं बैठकर किया करते.
एक ओर गंगा की अश्वेत जलधारा गरज के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती और दूसरी ओर क्रांतिकारी साहित्य का प्रभाव हमारी किशोर रंगों में खून की रफ्तार बढ़ा जाता. पानी का प्रचंड वेग एवं उसकी अथक गतिशीलता की छाप हमारे ऊपर सर्वाधिक पड़ी और शायद इसीलिए गंगा के तट का आकर्षण हम दोनों के मन में सदैव बना रहा.
एक शाम हम गंगा के तट पर बैठे अपनी क्रांति संबंधी कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि अचानक ही आकाश काले बादलों से पटने लगा. गंगा पार की बस्तियां धुधली पड़ने लगीं, हवा का वेग बढ़ गया और थोड़ी ही देर में बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से लगा आसमान फट जायेगा. क्षण भर में ही प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया था. इससे पहले कि हम उठकर वहां से शहर की ओर चल देते, बूंदाबांदी शुरू हो गयी थी और शहर के फूलबाग स्थिति 'एडवर्ड मेमोरियल हॉल' पहुंचते-पहुंचते जमकर वर्षा होने लगी थी. यहां आकर हमें मालूम हुआ कि साथ की बहुमूल्य पुस्तक 'हीरो एंड हीरोइन ऑफ रशिया' तो हम जल्दबाजी में गंगा किनारे ही छोड़ आए हैं.
रूस पर जारतन्त्र के विरुध्द रूसी युवक-युवतियों के सशस्त्र संग्राम की वह इतिहास-पुस्तक दुर्लभ होने के कारण हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान थी, लेकिन उस घने अंधकार में वर्षा के साथ प्रचंड वायु का वेग सम्भालता हुआ दो मील का रास्ता तय करके उसे लाये कौन. मेरे जाने की बात सरदार को नागवार सी लगी. शरीर में वह मुझसे निश्चित रूप से तगड़ा था और अपने उसी तगड़ेपन की दलील देकर उस वक्त उसने मुझे जाने से रोक दिया और खुद लम्बी डग भरता हुआ अंधेरे में गुम हो गया.उसे जाते हुए कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि मेरी भावुकता ने मुझे झिंझोड़ा और मैं भी उस बीहड़ अंधकार में सरदार के पीछे हो गया.
घने अंधकार में बेतहाशा भागते मेरे पैरों को अपने भागने का अहसास तब हुआ जब वे बीच सड़क पर बैठे सरदार से टकराये. सिर की रेशमी पगड़ी आधी खुलकर कीचड़ में सनी थी, एक हाथ से पुस्तक एवं दूसरे से अपने पैर का अंगूठा थामे वह लथपथ पड़ा था. पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था. पगड़ी चीरकर मैंने पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर सुरेश दा के मेस भीगते हुए वापस आया. उससे अलग अपने घर लौटकर मेरा मन सरदार के दुख से बेचैन था. मैं वहां से रूई-पट्टी, जैम्बक की डिबिया लेकर उसी मूसलाधार वर्षा में सरदार के पास पहुंचा, उसके अंगूठे का खून साफ कर उस पर मरहम पट्टी की और रात भर उसके पास बैठा रहा. सुबह होते ही घर के अनुशासन की सुधि आयी.
उस दिन परिवार से मिलने वाली तमाम यंत्राणाएं मैं धैर्यपूर्वक सह गया सिर्फ इस तसल्ली पर कि अपने प्रिय मित्र के प्रति अपना छोटा-सा कर्त्तव्य निभाया. और सरदार का वह स्नेहयुक्त आवेश- 'पीओ, देर न करो. तुम्हें पीना ही पडेग़ा. दूध वाले की दुकान के सामने गर्म दूध से भरा गिलास लिए वह मुझे आदेश दे रहा है. दूध से उन दिनों अरुचि नहीं थी लेकिन भरपेट भोजन के बाद पक्का आधा सेर दूध चढ़ा जाना मेरे पेट के लिए मुश्किल था. आज भी दिल्ली और आगरा स्थित दूध की दुकानों के दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं. उन्हीं दुकानों के मालिक बाद में हमारी उपस्थिति दिल्ली और आगरा में सिध्द करने के लिए हमारे मुकदमों में आए थे. दरअसल, भोजन के बाद गर्मागर्म दूध का गिलास चढ़ा जाने का पाठ मुझे सरदार ने ही दिया. जब कभी पैसा पास होता वह दूध पीने के विलास से नहीं चूकता था.
जहां रोटी का लुकमा भी निश्चित न हो वहां दुग्धपान विलास की ही श्रेणी में आएगा न? और उसे सिर्फ तीन पाव गर्मागर्म दूध से ही संतोष नहीं था बल्कि गिलास के दूध पर कम-से-कम डेढ़ छटांक मोटी मलाई का टुकड़ा भी अलग से पड़ना चाहिए. मलाई न रहने पर घी का तडका (छोंक) वह गर्म दूध में दे लेता था. शरीर में खून बढ़ाने का उसका यही उपयुक्त नुस्खा था.
दूध के प्रति एक असीम आसक्ति उसके मन में थी. स्वास्थ्य के प्रति वह कभी उदासीन न रहा, हालांकि बाद के पार्टी जीवन में नियमित रूप से हमें भोजन भी नसीब नहीं हुआ. विप्लवी जीवन की अनिश्चित परिस्थिति एवं जीवन-धारण के लिए सीमित साधन और व्यवस्था के अभाव में भी वह शरीर और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहा. यद्यपि जीवन के प्रति उसके मन में जबरदस्त आसक्ति थी, तथापि उसका कहना था कि जीवन जब अधिक सुंदर और प्रिय मालूम पड़ने लगे, तभी अपने आदर्श के लिए उसे बलिदान करना चाहिए.
संस्मरण की इस कड़ी के रूप में एक और दृश्य मेरी आंखों के सामने अब भी कौंध जाता है... कानपुर स्टेशन का जन-प्लावित प्लेटफार्म, 'जो बोले सो निहाल.... सत्श्री ..अ...का....ल...' के गगनभेदी नारे से दिग-दिगंत गूंज उठा है. गुरु के बाग के सत्याग्रही सिख मोर्चा डालने के लिए पंजाब जा रहे हैं. उन दिनों हर स्टेशन पर, जहां ट्रेन रुकती थी, अधीर जनता सत्याग्रहियों के दर्शनार्थ टूट पड़ती थी. प्रत्येक स्टेशन पर वीर सत्याग्रहियों को भोजन कराने के लिए लंगर खोले गए थे. कानपुर स्टेशन पर भी ऐसी ही व्यवस्था थी और सत्याग्रहियों की एक झलक लेने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी. फूलों और फूल-मालाओं की वर्षा! मैं भी स्टेशन गया था. अपार जनसमूह के बेग को ठेलकर सत्याग्रहियों के डिब्बों तक न पहुंच पाने की मजबूरी में ओवर-ब्रिज पर जाकर खड़ा हो गया और असंख्य सिरों से पटे प्लेटफार्म का दृश्य वहीं से देखने में तल्लीन था कि भीड़ को चीरती मेरी दृष्टि अपने सरदार मित्र पर पड़ी वही रेशमी पगड़ी और सफेद कमीज दोनों आस्तीनें बांह पर चढ़ी हुईं . एक हाथ में शरबत की बाल्टी और दूसरे में लंबा-सा गिलास. अपने कंधों से भीड़ को ठेलता हुआ वह सत्याग्रहियों के हाथों में शरबत के गिलास पकड़ा रहा था. भीड़ की खींचातानी में पगड़ी सिर से खिसककर कंधें पर लटक आई है जिसकी चिंता उसे नहीं थी. कम-से-कम समय में ज्यादा-से-ज्यादा सत्याग्रहियों की प्यास बुझा पाने की व्यग्रता उसके चेहरे, आंख और चाल में स्पष्ट देखी जा सकती थी.
ट्रेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी विश्रामहीन भाग-दौड़! मेरे प्रिय साथी सरदार का यह एक और रूप था. थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन चल पड़ी. फिर एक बार सत्श्री अकाल के नारे से आकाश गूंजा और कोलाहल मुखरित स्टेशन का प्लेटफार्म खाली होना शुरू हो गया. भीड़ पिघलने लगी. जो सत्याग्रहियों को देखने, उनसे मिलने-मिलाने आए थे, बाहर कीओर खिसकने लगे और बच गया हाथों में गिलास-बाल्टी लिए मेरा वह सरदार मित्र! मैं ओवर-ब्रिज से उतर उसकी बगल में खड़ा हुआ पर उसे जैसे किसी बात की सुध नहीं थी. ट्रेन जाने की दिशा में मंत्रमुग्ध आंखों में उदासी लिए अब भी वह खाली पटरी देखे जा रहा था. अपने कंधे पर मेरे हाथ का दबाव महसूस कर मुड़ा और मुस्कराकर एक हाथ से मेरे पंजे को दबाया बोटू .... उसकी आंखों में कोई अदृश्य निर्णय कौंध उठा था उस घड़ी. उस दिन लगभग गुमसुम और उदास वह जनशून्य स्टेशन से मेरे साथ बाहर हुआ था और फिर वह दिन भी आया जब दल के आदेशों पर उसे कानपुर, 'प्रताप', सुरेश दादा और मुझे छोड़कर एक छोटे स्कूल का हेडमास्टर बनकर अन्यत्र जाना पड़ा. विप्लव दल के नियमानुसार कुतूहलवश जरूरत से ज्यादा किसी का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए मना था और सरदार शायद सब दिन ऐसा अनुभव करता रहा था कि कोई रहस्य वह अपने एकमात्र एवं अनन्य साथी मुझसे छिपाता रहा है, वरना कानपुर से विदाई लेने के दिन ही क्या खुलता.
शिक्षक का पद ग्रहण करने जाते वक्त मुझसे मिलने आया था और हमारी आत्मीय घनिष्टता के बावजूद दल की मर्यादा रखने के लिए अब वह जिस रहस्य को छिपाये हुए था, विदाई के क्षण उसे व्यक्त किये बगैर न रह सका.
जिस तरुण बलवंत सिंह के स्नेहपाश में मैं अब तक बंधा था, वही सरदार भगत सिंह के रूप में मुझसे विदा ले गया. यही उसका असली परिचय था लोगों ने उसे बाद में विप्लवी सरदार भगत सिंह के रूप में जाना, लेकिन मेरे लिए तो वह सब दिन मानवीय गुण-सम्पन्न, भाव में गम्भीर भावुकता से ओतप्रोत बलवंत सिंह बना रहा. बाद की हमारी मैत्री परवर्ती क्रांतिकाल में एक-दूसरे के साथ सहयोगी की भूमिका, उसकी फांसी से लेकर मेरे जलावतन तक का प्रसंग इस कड़ी की अगली कहानी है.
सन् उन्नीस सौ सत्ताईस-अट्ठाईस का समय हमारे राष्ट्रीय जीवन में क्रांति के साथ-साथ संकट का काल भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्हीं दिनों हमारी आजादी की लड़ाई का स्रोत एक नये रास्ते की ओर प्रवाहित हुआ. उस वक्त तक देशवासी क्रांतिकारी आंदोलन और उसकी विचारधाराओं से ज्यादा परिचित नहीं थे और अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को साधारण खूनियों तथा डकैतों की श्रेणी में डालकर देश की जनता को सब दिन गुमराह करने का प्रयत्न करती रही थी.
ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि विप्लवी देश में संत्रास एवं अराजकता फैलाना चाहते हैं जबकि विप्लवी देश में परिवर्तन के प्रति आग्रही थे. जनसाधारण को विप्लवी के प्रति जागरुक बनाकरआर्थिक परिवर्तनों द्वारा शोषणविहीन समाज की स्थापना ही उनका लक्ष्य था. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि क्रांतिकारियों की ओर से देशवासियों के सम्मुख एक निश्चित कार्यक्रम पेश किया जाए और देश के नेताओं को असेंबली भवन के भीतर वैधानिक कार्यक्रमों के दांव-पेच से मुक्त कर जनांदोलन के प्रति उत्साहित किया जाए, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में अंग्रेज सरकार की ओर से भारत के लिए स्वायत्ता शासन की मांग बार-बार ठुकरा दी गयी थी. जन नेताओं के लाख विरोध के बावजूद यहां की जनता के मानवीय अधिकारों को विलुप्त करने के लिए केंद्रीय धारा सभा से टे्रड डिस्प्यूट बिल स्वीकृत करा लिया गया था. कानून स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के करोड़ों भूखे-मेहनतकश लोग अपनी आर्थिक दशा सुधारने के प्रारंभिक स्वत्व एवं एकमात्र उपाय हड़ताल से वंचित कर दिए गए थे.
केंद्रीय विधानसभा में हमारे जन-प्रतिनिधियों के उस अपमान और उस अमानुषिक बर्बरतापूर्ण कानून द्वारा देश की करोडों ज़नता पर जो हमला हुआ था उसी के विरोध में भारतीय क्रांतिकारी संस्था 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' द्वारा केंद्रीय असेंबली के सभाकक्ष में बम डालकर गोरी हुकूमत को एक चेतावनी देने के सुझाव पर आगरा हेड क्वार्टर में आलोचना गोष्ठी की बैठक चल रही थी.
असेंबली में बम डालकर आत्मसमर्पण करना एवं बाद में मुकदमे के दौरान अभियुक्त के कटघरे में खड़े होकर भारतीय क्रांतिकारी दल की ओर से विप्लवियों के विचारों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का दिग्गर्शन कराने के लिए एक विशद राजनीतिक वक्तव्य देने की सूझ सरदार भगत सिंह के मस्तिष्क की ही उपज थी. लेकिन इसे निभाये कौन? यानी केंद्रीय असेंबली में बमफेंकने जैसा जोखिम भरा कार्य कौन करे? इसे पूरा करने का सीधा एवं साफ अर्थ था मृत्यु!
लाख सावधानी के बावजूद असेंबली भवन के फर्श पर बम फटने के साथ किसी की मृत्यु की सम्भावना स्पष्ट थी और उसके बाद वहां नियुक्त सुरक्षा पुलिस या सार्जेंट द्वारा बम फेंकने वाले को तुरंत मौत के घाट उतार देना भी लगभग निश्चित ही था. बावजूद इसके कि हम सभी क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने की बलिदानी भावना से प्रेरित हो, प्रियजनों से नाता तोड़, किसी भी क्षण मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प ले, सिर पर कफन बांध, गृह-त्यागी बनकर निकल पड़े थे, फिर भी विचार गोष्ठी में बैठकर अपनी-अपनी सुरक्षा पर नजर गड़ाये दूसरे साथी को निश्चित मौत का फरमान सुनाना किसी के लिए भी संभव न था. ऐसा कोई व्यवहार किसी के भी मन को संदिग्ध बना सकता था.
सरदार ने सहर्ष आगे बढ़कर निश्चित मौत से खेलने का बीड़ा उठाया, साथ-साथ मैंने भी. वर्षों पहले कानपुर में गंगा के किनारे बैठे-बैठे जिन अनागत दिनों की कल्पनाएं हम बार-बार किया करते थे, कि एक साथ ही दोनों देश की स्वतंत्राता के लिए आत्माहुति देंगे, उसे साकार करने का समय आ गया था... हम दोनों- सरदार और मैं- बम के साथ आगरे से दिल्ली पहुंचे. लगभग महीने भर तक दिल्ली में ही टिके रहे. मैं हाफ पैंट, कमीज और जूता पहनता था और सरदार फ्लैट हैट लगाने लगे थे. प्रत्येक संध्या बम को अखबार में ढंककर कोट की नीचे वाली जेब में रखे हम साथ-साथ असेंबली भवन जाते, वहां का वातावरण परखते, पहरे पर संतरियों की गतिविधि देखते और अनुमान लगाते-कैसे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगें.
इसी बीच एक दिन सरदार ने साथ-साथ फोटो खिंचवाने की बात रखी. कुछ देर तो मैं टालता रहा, लेकिन सरदार जब जिद पर उतर आए तब मुझे भी झुकना पड़ा, और वही एकमात्रा तस्वीर हम दोनों की आखिरी यादगार बनकर रह गयी. फिर आया वह दिन जिसके लिए हम आगरे से चलकर दिल्ली आए थे और लगातार महीने भर तक बिना नागा असेंबली भवन के अगल-बगल चक्कर लगाते रहे थे. यानी 8 अप्रैल, 1928. दिन के ग्यारह बजे स्थान केंद्रीय असेंबली हॉल जिसे अब संसद कहा जाता है. ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर जनमत जानने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था. अध्यक्ष की कुर्सी पर सरदार बल्लभ भाई पटेल विराजमान थे. ट्रेजरी बेंचों पर सर जेम्स क्रेरर एवं सर जार्ज शुस्टर. विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वायसराय की सीट पर, दर्शक दीर्घा में, सर जान साइमन.
सरकारी बैंचों के सामने विरोधी सीट पर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदनमोहन मालवीय एवं डा. मुंजे आदि. बम हम दोनों ही की जेब में थे. ऊपर से पीछे की खाली बैंचों को लक्ष्य करके हमने बम फेंके. जोरों का धमाका हुआ, लेकिन चूंकि किसी को मारने का इरादा तो था नहीं, इसीलिए कमजोर बम बनाये गए थे ताकि धमाके पैदा करने के अलावा और किसी तरह का भयंकर, घातक या मारक प्रभाव उससे पैदा न हो सके. 'इंकलाब जिंदाबाद' एवं 'साम्राज्यवादी शासकों के बहरें (राष्ट्रीय मांगों के प्रति) कानों को खोलने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत है' के नारों एवं फटे बम के धुएं से हॉल भर गया और भगदड़ मच गयी. डर के मारे सर जेम्स क्रेरर बैंचों के नीचे जा छिपे.
बम के साथ फेंके गए लाल रंग के छपे पर्चें धुएं की सतह पर हॉल में इधर-उधर तैर रहे थे. उस पर्चें में गोरी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए भारतीय क्रांतिकारी दल के उद्देश्यों का स्पष्ट हवाला दिया गया था-'दो नगण्य इकाइयां (सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त) को कुचलने से राष्ट्र नहीं दबेगा... सरकार इस बात को समझे कि पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के विरुध्द जनमानस का विरोध प्रदर्शित करने के अतिरिक्त हम इतिहास को भी यह साक्ष्य देना चाहते हैं कि व्यक्तियों का दमन करना आसान है, लेकिन विचारधाराओं का दमन नहीं किया जा सकता. विशाल साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं लेकिन विचारधारा नष्ट नहीं होतीं. बोरबोन और जार का पतन हो गया, किंतु क्रांतिकारी आगे बढ़ते गए, हमें, जिनको मनुष्य जीवन से प्रेम है और जो एक बड़े ही गौरवमय भविष्य की कल्पना करते हैं, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्राता के लिए बाध्य होकर मानव-रक्त बहाना पड़ रहा है यह आवश्यक है क्योंकि जो मनुष्यता के लिए शहीद होते हैं, उनके त्याग से क्रांति की वह वेदी बनती है जहां से मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो सकेगा-इंकलाब जिंदाबाद'.
अपनी पूर्व योजनाओं के अनुसार एवं मार्शल लॉ जारी न हो या बम फेंकने के अपराध में निर्दोष व्यक्ति न पकड़ लिए जायें, हम दोनों ही ने आत्मसमर्पण कर दिया. तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने उस घटना का तात्पर्य अच्छी तरह समझा और बम विस्फोट के बाद ही व्यवस्थापिका सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण के समय चर्चा करते हुए बताया कि बमों का यह प्रकार किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक संस्था (अंग्रेजी शासन) पर किया गया है. हम दोनों को दिल्ली के दो अलग-अलग थाना में रखा गया.
मुकदमे शुरू हुए फिर हमारा स्थानान्तरण दिल्ली जेल में हुआ जहां एक साथ सटी दो अलग-अलग कोठरियों में हमें रखा गया. बीच में खड़ी अभेद्य दीवार. नियाज अली हमारा जेल वार्डन था जिसे एक अरसे तक हम हाड़-मांस का न होकर पत्थर का बना समझते रहे.
नियाज अली ने कभी मुझे और सरदार को एक साथ न होने दिया. स्पर्शानुभूति की बात तो दूर रही, उसने कभी हम दोनों को एक-दूसरे का चेहरा तक नहीं देखने दिया, उन दो-चार दिनों को छोड़कर जबकि इकट्ठे हमें अदालत ले जाया जाता था. दिल्ली की उस विशेष अदालत में न्यायाधीश के सामने प्रविष्ट होते समय अपने-अपने हाथ-पांवों में पड़ी बेड़ियां की झंकार के साथ हम 'क्रांति चिरंजीवी हो' का नारा लगाते. पूरा न्यायालय गूंज उठता था, और तभी से यह नारा राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त हो गया. बम विस्फोट के साथ पहले-पहल सरदार के मुंह से निकली 'इंकलाब जिंदाबाद' की घोषणा जैसे पूरे राष्ट्रीय जनजीवन में व्याप्त हो गयी.
मुकदमे के दौरान न्यायाधीश महोदय ने सरदार से 'क्रांति' शब्द की व्याख्या करने को कहा तो सरदार ने बताया- 'क्रांति या विप्लव खून-खच्चर ही का रास्ता नहीं, और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध का कोई स्थान है. बम और पिस्तौल ही क्रांति का धर्म हो, ऐसा भी नहीं है. क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान समाज और शासन व्यवस्था जो स्पष्टत: अन्याय एवं अत्याचारों पर आधारित है, परिवर्तित हो. आप पूर्ण परिवर्तन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें सर्वसाधारण की सत्ता कायम हो सके.'
आसिफ अली साहब ने हमारी ओर से वकालत की थी और हमारे गवाह बने थे डॉ. मुंजे एवं पंडित मदनमोहन मालवीय. न्यायालय ने हम दोनों को आजीवन काले पानी की सजा दी. 1930 में 'लाहौर षडयंत्र केस' के अंत में जब मैं सदा के लिए सरदार से बिछुड़कर मुलतान जेल भेज दिया गया, तब सरदार ने मेरी बहन को एक पत्र लिखा था जो आज भी मेरे जीवन की अमूल्य निधि है.
17 जुलाई, 1930 को लाहौर सेंट्रल जेल से लिखा गया वह पत्र सरदार के व्यथातुर हृदय की अभिव्यक्ति हैं-'बटुक की जुदाई आज मेरे लिए असह्य हो रही है. इस बिछोह से मैं एकदम स्तब्ध सा हो गया हूं... एक-एक पल मेरे लिए असह्य भार बन गया है. सचमुच, अपने भाई एवं परिजनों से भी ज्यादा प्रिय उस मित्र से अलग हो जाना आज मेरे लिए अत्यन्त ही कठिन गुजर रहा है...हमें सबकुछ धैर्यपूर्वक सहन करना है और आपसे भी हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करने का अनुरोध करूंगा .'
'लाहौर षडयंत्र केस' में जब सरदार को फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया तब अपने एक पत्र में उसने मुझे लिखा:
'प्रिय बटुक,
दीर्घकाल तक हम लोगों का विचार-प्रहसन चलने के बाद अब उस पर यवनिका पात हुआ. न्यायाधीशों ने सजाएं घोषित कर दी हैं और उन सजाओं की इत्तला हमें भेज दी गयी है. मुझे फांसी की सजा मिली है. तुम्हें मालूम है कि मैं लाहौर जेल की उन्हीं फांसी की कोठरियों में हूं, जहां चंद रोज पहले तुम मेरे साथ थे. इन फांसी की कोठरियों में कुल पैंतालीस मृत्यु-दंड प्राप्त बंदी हैं जो प्रतिक्षण अपनी अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वे अभागे बन्दी फांसी के फंदे से छूट पाने के लिए दिन-रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. उनमें से अधिकांश अपने कृत्यकर्म के लिए अत्यंत ही अनुलप्त हैं और इन अभागे बन्दियों के बीच मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, भगवान के बदले अपने आदर्शों में ही जिसकी अविचल आस्था है, एवं जिस आस्था के लिए मैं मृत्यु का आलिंगन करने जा रहा हूं, इसके लिए संतुष्ट हूं. तुमसे मेरा बिछोह अत्यंत ही पीड़ादायक है, लेकिन इससे कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होगी. मैं फांसी के तख्ते पर अपना प्राण विसर्जित कर दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रांतिकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुशी-खुशी आत्म-बलिदान कर सकता है. मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए जीवित रहोगे और मेरा दृढ़विश्वास है कि तुम यह सिध्द कर सकोगे कि विप्लवी अपने उद्देश्यों के लिए आजीवन तिल-तिल कर यंत्राणाएं सहन कर सकता है. मृत्यु दंड पाने से तुम बचे हो और मिलने वाली यंत्राणाओं को सहन करते हुए दिखा सकोगे कि फांसी का फंदा, जिसके आलिंगन के लिए मैं तैयार बैठा हूं, यंत्रणाओं से बच निकलने का एक उपाय नहीं है. जीवित रहकर विप्लवी जीवन भर मुसीबतें झेलने की दृढ़ता रखते हैं.
तुम्हारा-भगत सिंह'
सरदार अपने विचारों या व्यवहारों में कट्टरपंथी कभी नहीं रहे मस्तक पर सिख धर्म के द्योतक लंबे बाल, कंघा, कच्छा और कड़ा लेकर वह कानपुर आए थे, लेकिन बाद के दिनों में परिस्थिति के अनुसार उन्होंने खुद को दूसरे रूप में ढाल दिया. लंबे-लंबे बाल कटवाकर नीचे से ऊपर तक सूट एवं हैट से लैस उन्होंने अंग्रेज साहबों का रूप धारण किया. हिंसा एवं अहिंसा की उधेड़बुन में उनके विचार उलझे हुए नहीं थे, न ही उनके मन में कभी किसी के प्रति हिंसा या द्वेष पनपा. राजनीतिक बंदियों को युध्दबंदी (प्रिजनर ऑफ बार) की स्वीकृति दिलाने एवं तदनुसार उनके सम्मानपूर्वक व्यवहार की मांग पर बंदियों द्वारा सामूहिक अनशन का संग्राम आरम्भ करना तथा उसी संग्राम के द्वारा देश की मुरझाई हुई चेतना में फिर से स्पंदन जगाने की कल्पना सरदार ने ही की थी और उसी संग्राम के फलस्वरूप पूरे देश में एक अभूतपूर्व परिस्थिति उत्पन्न हुई एवं बाद में 1930 का जनांदोलन जिससे प्रेरित हुआ. खुद सरदार ने जेल के भीतर 14 जून, 1929 से प्रारंभ करके लगातार 127 दिनों तक भूख की अनन्त ज्वाला में घुलते हुए मौत की प्रतीक्षा की थी...
गंभीर मननशीलता, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं आत्मबल पर अटूट विश्वास सरदार के अन्य गुण थे. दूसरे देश के क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ पराधीन भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का तुलनात्मक विचार सरदार के चिंतन का एक विशिष्ट पक्ष था.
***