Tuesday, December 29, 2009
सतभाया का शेष
उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में एक पंचायत है सतभाया..। इस पंचायत में कभी सात गांव हुआ करते थे। और रकबे की ज़मीन थी ३२० वर्ग किलोमीटर। अब बचे हैं डेढ़ गांव और सौ वर्ग किलोमीटर से भी कम का रकबा।
अपने साप्ताहिक धारावाहिक डॉक्युमेंट्री शूट करने के दौरान वहा गया तो दिल धक्क से रह गया। वहां की हालत देखकर। अब वहां गोविंदपुर, खारीकुला, महनीपुर और सारापदा समेत पांच गांव पूरी तरह समुद्र की पेट में जा चुके हैं। कानपुरु आधा डूब चुका है और सतभाया आखिरी सांस लिए समंदर के आगे बढ़ जाने की बाट जोह रहा है।
समुद्र ने गांव की खेती लायक १०६१ एकड़ ज़मीन, घर-बार सबकुछ निगल लिया है। और अब भी वह रुका नही है दिन ब दिन आगे ही बढ़ रहा है। दुनिया ग्लोबल वॉर्मिग की वजह से मालदीव किरिबाती तुवालू और पापुआ न्यू गिनी के डूब जाने का खतरा शायद कुछ दशक दूर हो, लेकिन सतवाया के गांव वाले चढ़ते समंदर का कोप झेल रहे हैं और यह विपदा शायद और भी घनी हो, जबकि उत्सर्जन के लिहाज से यह गांव बिलकुल पाक साफ है।
गांब में बिजली नहीं पहुंची है। एक मोटरसाइकिल तक नहीं। लेकिन आगे बढ़ते समंदर का कोपभाजन बना हुआ है गांव। सतवाया के लोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ज़रा भी योगदान नहीं करते.। फिर भी हाशिए पर पड़े इन लोगों पर कुदरत की मार पड़ी है। गांव रके बुजुर्ग बताते हैं कि पहले उन्हें समुद्र देखने के लिए तीन मील आगे जाना होता था, लेकिन अब समुद्र गांव के लिए खतरा बन गया है।
हृषिकेश विस्वाल गांव के ७८ साल के किसान हैं। उनके मुताबिक उनका गांव समुद्र में डूब चुका है। और वह बीस बरस पहले तक समुद्र देखने जाते तो वापसी में शाम हो जाया करती थी।
उत्कल विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्राध्यापक जी के पंडा कहते है कि सतभाया का डूबना ग्लोबल वार्मिंग का या दूसरे शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन का नतीजा है।
गांव का सवा सौ साल पुराना स्कूल, और बाकी इमारतें डूब गई हैं। अब कानपुरु के लोग भीतरकनिका नैशनल पार्क की सरहद में जंगल में नए बसेरे में रहते हैं,वहीं प्राइमरी स्कूल भी झोंपड़े में चलता है। लेकिन यह गांव भी समंदर की जद से दूर नहीं।
सतभाया और समंदर के बीच रेत का एक टीला है। लेकिन यह टीला कब तक गांव को बचा पाएगा? खुद टीले की रेत फूस के झोंपड़ों पर गिर कर नई मुसीबत बन रही है।पहले ही उड़ीसा का यह हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे था लेकिन विकास की कुछ कोशिशें हुईं भी तो समंदर के पेट में चली गईं। पहले गांव में छह टयूब वेल थे लेकिन उनमें से पांच समंदर में समा गए।
ऐसे में गांव में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई हैं। बचे खुचे हैंड पंप पानी तो देते हैं लेकिन उनमें से निकलने वाला पानी भी नमकीन और खारा हो चुका है। आज पूरे गांव में फूस के ढांचे बचे हैं। पक्की इमारत के नाम पर बस ढाई सौ साल पुराना पंचवाराही मंदिर और नया बना पंचायत भवन हैं। हर साल तकरीबन 300 मीटर की दर से आगे बढ़ रहे समंदर के पानी ने सतवाया पंचायत के पांच गांवो को अपनी चपेट में ले लिया है। पिछले साल यह गांव के 80 मीटर ज्यादा पास आ गया आया था। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए समंदर ने गोविंदपुर, खारीकुला, महनीपुर सारापदा समेत पांच गांवो को भारत के भौगोलिक नक्शे से मिटा दिया।
जारी
Thursday, December 17, 2009
कविताः ट्रिकल डाउन
मनमोहिनी मुद्रा में,
दिया बयान
धनकुबेरों को होने दो और भी धनी
उनके टैंकर में जब भर जाएगा मनी,
रिस-रिसकर पहुंच जाएगा आखिरी आदमी तक भी.
.जैसे सरपंच-मुखिया के खेतों को सींचने के बाद,
कलुआ-मधुआ के खेतों तक भी पहुंच जाता है पानी,
सीधे न पहुंचे तो,
माटी से रिसकर पहुंच तो जाता ही है
एक दिन,
रुपयों की बारिश से
उफनकर आता पानी
भर देगा
हर घर के आंगन को,
फूस की छत से टपकेगें सिक्के,
चूएंगे डॉलर
हर आदमी के पास होगी,
पैसो की तलैया,
जैसे बंगाल के गांव में हर घर के पीछे होता है
छोटा-सा डबरा,
जिसमें तैरती रहती हैं बत्तखें
देश बन जाएगा
डॉलर का महासागर,
लेकिन महासागर के बीच में जा पाएंगे,
सिर्फ बड़े जहाज,
हम जैसे नारियल के सूखे फल...
किनारे पर पड़े लहरो से टकराते रहेगे,
कभी सूखी रेत पर
कभी पानी में
आते-जाते रहेगे,
लगता है
रिस-रिसकर रस पहुंचाने की थ्योरी
रसहीन और अनमेल है
डाउन थ्योरी में
डाउन जाने का सिस्टम फेल है।
Tuesday, December 1, 2009
कविता- तू मेरा इतिहास
Sunday, November 22, 2009
गुस्ताख का रिटायरमेंट प्लान
हम भी वहीं खड़े थे,-" का कक्का, अमिताभ की बागबान देख आए हो क्या? "
-"अरे नहीं बचुकिया, दुष्यंत कुमार की एक ग़ज़ल पढ़ आया हूं..सो अचानक चिंता बढ़ गई है। "
"कौन सी ग़ज़ल कक्का?"
"अरे बुढापे पर बड़ी मार्मिक ग़ज़ल कही है, दुष्यंत ने। हमारे ज़माने के शायर थे। सुन लो....
लगने लगा है बिस्तर बाहर दालान में,
बूढे के लिए अब नहीं कमरा मकान में ,
दी थी जिन्हें ज़बान वो जवान हो गए ,
कहते हैं लगा लीजिए ताला ज़बान में,
रोटी बची है रात की सालन नहीं बचा
देकर गई है बेग़म कह कर ये कान में,
जान उसके जिस्म से जब निकल गई
बेटे ने मकबरा बनाया है शान में
हां कक्का कह तो आप सही ही रहे हैं...कनाडा वाले उड़नतश्तरी और दिल्ली वाले डॉ अनुराग को भी सुना दीजिए। मुमकिन है वह भी अपने बुढापे का कुछ इंतजाम कर लें।
कक्का मेरी तरफ मुडे, --"क्यों बे, अपनी सोच तूने क्या इंतजाम कर रखा है। उड़नतश्तरी और डॉ अनुराग की मत सोच। डॉक्टर तो फिर भी उम्रदराज़ (?) हैं, लेकिन उड़नतश्तरी तो माशाअल्लाह जवान हैं.. खुद बूढा़ हो रहा है, बाल तेरे सफेद हो गए, जो बचे हैं उनको लेमिनेट करवा ले। यादें रह जाएंगी तो देख-देख कर आहें तो भर पाएगा...
हम हुमक उठे, --"क्या कक्का, अभी तो हमने बड़ी-बड़ी शरबती आंखों और रेशमी जुल्फों वाली मादक मादा की खोज ही शुरु की है..बुढापे की बात मत करो। गोपालप्रसाद व्यास भी तो कह गए हैं..
हाय न बूढा कहो मुझे तुम,
शब्दकोष में प्रिये और भी
बहुत गालियां मिल जाएंगी
गुस्ताख मुस्कुरा उठा..। उम्र बढती है तो विनय बढ़ता है..।
बालों में छा रही सपेदी,
रोको मत उसको आने दो
मेरे सिर की इस कालिख को
शुभे स्वयं ही मिट जाने दो...
झुकी कमर की ओर न देखो,
विनय बढ़ रही है जीवन में
तन में क्या रखा है रुपसि,
झांक सको तो झांको मन में...
कक्का खिसिया गए, --बच्चा. अभी बच्चे हो मान लिया लेकिन रिटायरमेंट का प्लान तो करो...जो हम भुगतने से डरे और मरे जा रहे हैं तुम पर ना आए..
हमने कहा कक्का, अभी अरुणाचल गए थे। वहां देख आए हैं, दिहांग नद के किनारे झोंपडा बनाकर मछली मारुंगा.. गोवा में भी अच्छा है.. समंदर के किनारे टीन की शेड डाल दूंगा... जिदंगी कट जाएगी। वैसे अच्छा ऑप्शन तो बिहार के अपने गांव में लौटकर खटाल अर्थात् गऊशाला खोल देने का है। सात-आठ गायें और उतनी ही भैसे पोस लूंगा, दूध बेचेंगे घी खाएंगे....
और घी खाने के लिए चार्वाक की तरह कर्ज लेने की भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी। कक्का, .. कहीं सचिन के एड वाले एक्शन प्लान से प्रेरित तो नहीं हो रहे आप? वैसे भी-पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात् पूत कपूत हो संचित धन की वाट लगा देगा। पूत सपूत हो चो उसके लिए धन संचित करने की ज़रुरत ही क्या।
कक्का को असह्य हो रहा था, सीधे सिर पर चपत मारी कहा, तुम उल्लू हो, गधे भी..और अपनी राह ले ली।
पाठकों आप ही बताइए, रिटायरमेंट का प्लान ज़रुरी है? अगर है तो क्या करना चाहिए ....
Friday, November 20, 2009
क्योतो से कोपनहेगन

अपनी ज़मीन और हवा को साफ-सुथरा रखने का यह पहला मामला नहीं था।
जिन दिनों इंगलैंड में आद्योगिक क्रांति अपने शबाब पर थी, उन्हीं दिनों 1824 में फ्रांस के साइंसदान जोसेफ फुरियर ने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया।
1896 में स्वीडन के रसायनशास्त्री स्वांते अरहेनियस हों या 1938 में ब्रिटिश इंजीनियर गे कैलेंडर, विद्वानों ने पर्यावरण के लिए नुकसानदेह ग्रीन हाउस इफैक्ट के प्रति आगाह करना शुरु कर दिया था।
सन 1965 में पहली बार किसी सरकार ने पर्यावरण पर सलाह देने का काम कि.या और अमेरिकी सलाहकार समिति ने ग्रीन हाउस गैसों को चिंता का कारण बताया।
1972 में स्टॉकहोम में पहला जलवायु सम्मेलन हुआ। पर्यावरण को लेकर जाकरुकता की शुरुआत भी हुई। फिर 1988 में मांट्रियल प्रोटोकॉल सामने आया, जिसमें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन और एचएफसी यानी हाइड्रोफ्लोरो कार्बन के कम उत्सर्जन का संकल्प लिया गया था।
1992 में रियो डि जिनेरो मे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, लेकिन चिंताएं बरकरार रही। फिर,मौसम परिवर्तन के ख़तरों से निपटने के लिए 1997 में जापान के क्योटो में यह तय हुआ कि अलग-अलग चरणों में विकसित, विकासशील और पिछड़े देश तापमान बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले गैसों का ऊत्सर्जन कम करेंगे।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत चालीस औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए 1990 के आधार पर मानक तय किए गए । भारत और चीन जैसे विकासशील देशों पर यह पाबंदी बाध्यकारी नहीं थी। अब तक 184 देश इस पर अपनी सहमति जता चुके हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले अमेरिका ने अब तक क्योटो संधि को लागू नहीं किया है।
अमेरिका अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है कि प्रोटोकाल के तहत विकासशील देशों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। उसकी दलील है कि चीन और भारत जैसे देशों पर भी बाध्यकारी पाबंदियां होनी चाहिए।
अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने की कोई तय सीमा मानने को तैयार नहीं, वहीं भारत,चीन और ब्राजील जैसे देश विकसित देशों की और उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे में मामला पहले आप-पहले आप पर फंसा हुआ है।
भारत और चीन की दलील है कि उनका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विकसित देशों की बनिस्पत काफी कम है और इस वक्त उत्सर्जन पर रोक लगाना विकास पर पाबंदी जैसा होगा।
चीन और भारत दोनों का मानना है कि विकसित देशों और विकासशील देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती के मानक अलग-अलग होने चाहिए, हालांकि विकासशील और विकसित देशों का यह विवाद पुराना है और जलवायु परिवर्तन की हर बैठक में उठता रहा है।
अमरीका और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र के क्योतो प्रोटोकॉल पर सिर्फ़ इसीलिए हस्ताॿर नहीं किए क्योंकि वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसमें भारत और चीन के लिए कार्बन गैस उत्सर्जन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और यह भी एक सच है कि इस समय कार्बन गैसों के उत्सर्जन में चीन का नंबर अमरीका के बाद दूसरा है।
लेकिन चीन का तर्क है कि अमीर देशों के अब तक किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से ही जलवायु परिवर्तन हुआ है.
इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,--आईपीसीसी-- में रखे गए अपने प्रस्ताव में चीन धनी देशों के ग्लोबल वार्मिंग में योगदान का उल्लेख रिपोर्ट में चाहता है। चीन के मुताबिक 1950 से पहले अमीर देश 95 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार थे, जबकि 1950 से 2000 के बीच वे 77 प्रतिशत गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, ऐसे में उत्सर्जन कम करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों पर होनी चाहिए। उधर, विकसित देश चीन की इस दलील से सहमत नहीं हैं।
अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय संघ भी चाहता है कि विकासशील देशों को भी इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यूरोपीय संघ मानता है कि विकासशील देश धनी देशों को दोषी ठहराना छोड़कर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए प्रयास करना शुरु करें।
यानि मामला अब भी वहीं अटका है जहां क्योटो में था।
लेकिन उत्सर्जन अभी भी जारी है।
अब तक क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत समेत 184 देशों ने दस्तखत किए हैं,जो कुल 70 फीसदी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। 16 फरवरी 2005 से इसे दस्तख्वत करने वाले सभी देशों ने लागू कर दिया है। लेकिन दुनिया की 35 फीसदी ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले अमेरिका ने इसे लागू नहीं किया।
डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाली युनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में अब तक के हालात की समीॿा के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस साल अक्टूबर मेंो बैंकॉक में हुई क्लाइमेट चेंज टॉक में क्योटो प्रोटोकॉल को तकरीबन खारिज करने वाले अमेरिका का कोपेनहेगन में क्या रवैय्या रहता है।
भले ही देशों के बीच तकरार जारी है लेकिन इस बार अपने मतभेदों को दूर कर सबको इस बात पर सहमत होना चाहिए कि धरती को जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से कैसे बचाया जाए।
उम्मीद करनी चाहिए की कोपनहेगन में देशों के बीच आम राय बनेगी, क्योंकि वक्त हाथ से निकला जा रहा है।
Wednesday, November 18, 2009
गरम होता धरती का मिजाज़
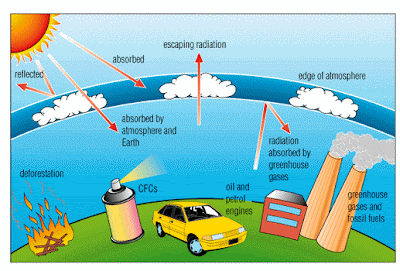
धरती को सूरज से प्रति वर्ग मीटर ३४३ वाट सौर विकिरण मिलता है। ऊर्जा की यह मात्रा बहुत ज्यादा है, हमारी कायनात को जलाकर राख कर देने के काबिल...लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि इस ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा अंतरिक्ष में वापस चला जाता है।
सूरज से आने वाली किरणों का करीब तीस फीसद हिस्सा बादलों से टकरा कर अंतरिॿ में वापस लौट जाता है। करीब बीस फीसद हिस्सा धरती की कुदरती कामकाज यानी पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण , और दूसरी भौतिक-रासायनिक बदलावों में खर्च होता है।
बचे हुए 50 प्रतिशत विकिरण में से तकरीबन 49 फीसद हिस्से को धरती की सतह सोख लेती है और और फिर उसे इंफ्रारेड किरणों यानी ताप किरणों में बदलकर वापस अंतरिक्ष में भेज देती है।
लेकिन हमारे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइ ऑक्साइ़ड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड और जलवाष्प इस ऊर्जा को रोकने का काम करती हैं। ऐसे में वायुमंडल में इन गैसों मौजूदगी बढ़ने से धरती गर्म हो रही है तय है। तापमान में इस बढो़त्तरी से ध्रुवों पर बर्फ तेजी से पिघलती है जिसके साथ शुरु होती है प्राकृतिक असंतुलन की एक लंबी श्रृंखला।
इस मुश्किल की शरुआत हूई 18 वीं सदी में यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद से। पूरी दुनिया में तेजी से कल कारखानों का विकास हुआ और हमने वायुमंडल में धुआं और दूसरी जहरीली गैस छोड़नी शुरु कर दीं।
हवा को जहरीला बनाने के साथ ही धरती द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी जा रही इंफ्रारेड ताप किरणों का पहले से ज्यादा हिस्सा इन गैसों की वजह से वायुमंडल में ही रुकने लगा है। धरती का बढ़ता तापमान इसी प्रक्रिया का नतीजा है।
पृथ्वी का औसत तापमान 18 वीं सदी के बाद अब तक 0.6 डिग्री सेन्टीग्रेट तक बढ़ गया है। समुद्र का जलस्तर बीसवीं सदी में औसतन 10 से 20 सेमी तक बढ चुका है। 21वी सदी के पहले दशक के अंत तक इस स्तर में 10 सेमी और इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है।
धरती के गरम होते जाने से आर्कटिक की बर्फ लगातार पिघल रही है।
अनुमान है कि बीसवीं सदी के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सात फ़ीसदी बर्फ पिघल चुकी है। हिमालय की चोटियां भी इसकी जद से दूर नहीं.....
ग्लेशियर हर साल घटते जा रहे हैं जिससे बाढ़ औरभूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका भी पहले से काफी ज्यादा हो चुकी हैं।
हिमालय की बर्फ पिघलने की अगर यही रफ्तार रही तोे मैदानी इलाकों को सींचने वाली नदियों में पहले बाढ़ आएगी और फिर वो सूखने के कगार पर पहुंच जाएंगी। भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यामां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
जलवायु परिवर्तन की अगली मार होगी खाद्यान्न के उत्पादन पर, धरती के गर्म होने से गेहूं और धान की पैदावार पर असर पड़ेगा और फसल चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा।
जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीकी देशों में होने वाली खेती में दिक्कतें आएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर उन छोटे किसानों पर पड़ेगा जो कई पीढ़ियों से खेती के लिए मौसमी बरसात पर ही निर्भर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले दशकों में बरसात के पैटर्न में बदलाव आएगा और इसके चलते खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से गिरावट आएगी।
समस्या ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर उस आबादी पर पड़ेगा जिसका वैश्विक तापमान बढ़ाने में सबसे कम योगदान है।
Tuesday, November 17, 2009
पर्यावरण परिवर्तनः प्रलय की ओर

हम धरती की आबोहवा को इसी तरह ज़हरीला बनाते रहे तो विनाशकारी गतिविधियों के शुरु होने के जिम्मेदार हम खुद होंगे। अगर कुदरत से चलने वाली छेड़छाड़ इसी तरह जारी रही तो ये सब हकीकत में बदल सकता है।
हमारे आस पास चिड़ियों का चहचहाना कब कम हो गया, देखते देखते कैसे पेड़ कटकर हमारे घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में तब्दील हो गए, कभी रात में साफ़ दिखने वाले तारों और हमारे बीच कैसे एक झीना सा धुंध का पर्दा आ गया, कैसे नदियों में आम तौर पर पानी कम हो गया या नदियों का रंग ही बदल गया ... और कैसे कभी पड़ोसी की अलग सी दिखने वाली गाड़ी हमारी और हम जैसे बहुत से लोगों की गाड़ियों की भीड़ में गुम हो गई।....
इंसान के शरीर की तरह धरती का भी अपना एक सामान्य तापमान होता है। पृथ्वी का ये औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लेकिन इस सदी के आखिर तक इसके 6 डिग्री बढ़ने की आशंका है। तापमान में ये इजाफा दुनिया के भूगोल और पर्यावरण दोनों को बदल कर रख देगा।
जारी
Saturday, November 14, 2009
बीस साल बाद

बीस साल पहले याद है मुझे, मैं प्राइमरी में पढ़ा करता था। तब, भी क्रिकेट को लेकर यहीं जुनून था। बड़े भाई साहब क्रिकेट खेलते भी थे, क्रिकेट सम्राट नाम की पत्रिका भी घर में आती थी। तो सचिन तेंदुलकर और अमोल मजूमदार नाम के दो शख्सों से परिचय हुआ। चौथी कक्षा में पढ़ता था, पाठ्य-पुस्तकों से ज्यादा मन क्रिकेट सम्राट में लगता था।
सचिन का चयन टीम में हुआ था। लेकिन स्कूल के दिनों मे मेरा दोस्त सचिन की बजाय अमोल को ज्यादा टैलेंटेड बताता रहा। लेकिन शारदाश्रम के इस बच्चे को लेकर मेरे मन में एक मोह-सा हो गया।
कुछ दिनों बाद भाई ने बताया कि पहले टेस्ट मैच मे यह लड़का कुछ खास नहीं कर पाया..पहले वनडे में भी सिफर। फिर भी मन नहीं माना।
बड़े भाई साहब उन दिनों वेंगसरकर, शास्त्री और कपिल के दीवाने थे। अज़हर की कलाई की लोच पर फिदा थे, और मैदान पर अज़हर जैसा ही दिखना और खेलना पसंद करते थे। लेकिन फिर हमने अखबार में पढ़ा कि सचिन नाम के इस लडके ने अजीबोगरीब एक्शन वाले अब्दुल कादिर के धुनक दिया। मेरे मन को ठंडक पहुंची।
सचिन का कारवां बढ़ निकला था। मेरे खपरैल घर में सचिन का एक पोस्टर विराजमान हो गया। सन ९१ का साल था, बूस्ट वाला कोई विग्यापन था। गले में सोने की चेन, घुंघराले बाल। सोफे पर पसारा हुआ सचिन..। उन दिनों नवजोत सिंह सिद्दू ६ शतक मार कर वनडे भारतीय बल्लेबाज़ी में शीर्ष पर थे। उनका लाठीचार्ज मशहूर हुआ करता था।
सन ९४ में सिंगर कप में सचिन का पहला शतक आया तो हमने यही सोचा कि क्या यह सिद्धू के ६ शतकों की बराबरी कर पाएगा? डेसमंड हेंस के १७ शतकों को तो हम अजेय मान चुके थे। उन दिनों सचिन की तुलना अपने समकालीनों इंजमाम और लारा से होने लगी थी।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए मुझ अपने ब्लॉग पर लिखने की ज़रुरत नहीं। सारे समुद्र के पानी को स्याही बनाकर और सारे जंगलों की लकड़ी को कलम बनाकर सारी पृथ्वी क कागज बना कर पीटर रीबॉक से लेकर गावस्कार तक ढेर सारा लिख चुके हैँ। कमेंट्री में जेफरी बायकॉट वॉट अ शॉट, वाट अ शॉट चिल्ला-चिल्ला कर अपना गला बैठा चुके हैं।
लेकिन मुझे साल ९८ का शारजाह याद है। सेमिफाइनल में १४३ और फाइनल में १३६ बनाकर जीतने वाले सचिन की तारीफ में उन्ही के हाथों कुटने-पिसने वाले वॉर्न और माइकल कास्परोविच ने पुल नही फ्लाई ओवर बांध दिए। हमारी सहयोगी विनीता उनकी बड़ी फैन हैं। कहती हैं, जबतक सचिन क्रीज पर रहता है, जीत की उम्मीद बंधी रहती है। वह इसकी ताकीद करती हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले मैच का हवाला भी देती हैं, जिसमें सचिन ने १७५ रन ठोंके थे।
बहरहाल, मैं कोई सचिन के आंकडो का बड़ा जानकार नहीं। लेकिन उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़ाव का कायल हूं। सचिन और रहमान जैसी बड़ी शख्सियते मुझ पर असर करती हैं, और उन्हें मिलता हुआ सम्मान मुझे खुद को मिलता सम्मान लगता है। कई बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सचिन किसी की रगो में एड्रिनलीन दौड़ाने के लिए काफी नहीं है?
Friday, November 13, 2009
झारखंड: पैंतरा दोनों ओर से है..
 एक-दूसरे को कोसते-कोसते भाजपा पलट जिन भाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस की ताजा दोस्ती हुई है, उसका हश्र क्या होगा? सूबे में इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है।
एक-दूसरे को कोसते-कोसते भाजपा पलट जिन भाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस की ताजा दोस्ती हुई है, उसका हश्र क्या होगा? सूबे में इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है।सही उत्तर तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन कांग्रेस और बाबूलाल कि निष्ठा को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
कहने वाले तो कहते हैं, जब कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन की न हुई, जब आरजेडी वाले लालू यादव और एलजेपी वाले रामविलास पासवान की नहीं हुई तो बाबूलाल किस खेत की मूली है।
पलटवार यह कि जिस संघ की हाफ पैंट की बदौलत झोलाछाप मास्टर से ऊपर उठकर बाबूलाल भाजपा के भग-वे के भरोसे केंद्र में मंत्री बने, राज्य के मुख्यमंत्री बने, वे जब उसके न हुए तो कांग्रेस के नीचे कब तक रहेगे?
अर्थात्, पैंतरा दोनों ओर से है..।
Wednesday, November 11, 2009
मेरा हंसना भारी पड़ रहा है...
कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं, जब आप रोना चाहते हैं..बुक्का फाड़कर। लेकिन रो नहीं सकते..क्योंकि आपकी रेपुटेशन ही नहीं है, उदास दिखने की। हर गम में खुश दिखना होता है, जोकर की तरह। मेरे साथ यही मुश्किल है। लाल दंत मंजन छाप दांत दिखाने की ऐसी आदत है कि लोग-बाग ज़रा सीरियस होते ही पूछ बैठते हैं- क्या बात है, उदास हो?
हर बात पर हंसो, तो दोस्त ताना देते हैं मेरी बात पर सीरियस नहीं हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो?? क्या किया जाए। मौलिक कैसे बना जाए?
कभी एक शेर स सुना था- बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, फकत इस वास्ते जिंदादिली से काम लेते हैं... एक और था ऐसा ही, ..... मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं वाला।
लेकिन, मजाक-मजाक में जिंदगी का आधा हिस्सा निकल लिया..। डॉक्टर भी कुछ दूसरे किस्म की सलाहें दे रहे हैं..। अपने आसपास से गजब के लोगों को जाते देख रहा हूं, मानता हूं मेरी उम्र अभी मरने की नहीं। लेकिन मरने की कोई खास उम्र भी होती है क्या?
लोगबाग धरती की गरमाहट से हवा की सनसनाहट और राजनीति से लेकर पता नही क्या-क्या डिस्कस कर ले रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है..। खुद पर से भरोसा उठता जा रहा है..।
कुछ दोस्त भी साथ छोड़ रहे हैं, कुछ ने ताजिंदगी दोस्त बने रहने का वायदा किया ज़रुर है पर हमने वायदों पर से यकीन करना छोड़ दिया है। दिल में कई ऐसी बाते होती हैं, जो किसी को भी नहीं बता सकते बेहद करीबी दोस्तों को भी नहीं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनपर आप सिर्फ आप खुद से बतिया सकते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों से घिरा बैठा हूं.. अभिमन्यु की तरह..
ऐसा नहीं कि नौकरी का संकट या दफ्तर का तनाव है.. वहां मिल रही कामयाबियां निजी जीवन में असीम मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। बस मन में आया तो लिख मारा।
अजीत राय ने मेसेज किया था, उनने भी ब्लॉग बना लिया है, यायावरकीडायरी.ब्लॉगस्पॉट.कॉम..खोजने पर भी नहीं मिला।
Friday, November 6, 2009
अब कौन करेगा कागद कारे?
कल रात को भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था। सचिन को बेलौस खेलता देख रहा था, उसके छक्के और चौकों की बरसात देख रहा था। भतीजे मनीष ने भैया से कहा, अब कल अंकल जनसत्ता का पहला पैज फाड़कर लाएंगे। जिसमें प्रभाष जोशी सचिन तेंदुलकर के लिए पन्ने रंगे रहेगें।
सचिन ने ताबड़तोड़ १७५ रन बनाए.. लेकिन ...
आज जनसत्ता खाली-खाली सा था। उदास, पितृहीन बालक की तरह।
दफ्तर गया तो अरविंद चतुर्वेदी प्रभाष जी का पुराना इंटरव्यू लॉग कर रहे थे। सवाल था कि प्रभाष जी आप इस उम्र में देशाटन पर क्यों रहते हैं?
बकौल प्रभाष जी, वह देशाटन पर रहते हैं तो यमराज के दूतों को छकाते हैं। यमदूत दिल्ली आते हैं , तो वह भोपाल मे होते हैं, यमदूत भोपाल पहुंचते हैं तो वह कालाहांडी में होते हैं.....
आईआईएमसी में हमें पढाने आए ते प्रभाष जी तो उनने हमें जानपांडे बनने को कहा था। जानपांडे ऐसे लोग होते थे जो धरती के कंपन को महसूस कर यह जान लेते थे कि वहां कुँआं खोदने से पानी निकलेगा या नहीं। उनका कहना था कि हमें समाज का जान पांडे बनना होगा।
उनकी किताबों और आलेखों और पत्रकारिता के काम पर लिखने वाला उचित आदमी नहीं मैं। यह किसी बड़े आदमी के जिम्मे हो। हमारे लिए प्रभाष जी प्रकाश स्तंभ थे, जिनके ज़रिए हमें सही रास्ता दिखता था।
बहरहाल, उनके तमाम स्तंभों में हम क्रिकेटीय स्तंभ कासकर पढ़ते थे। भारतीय क्रिकेट के लड़कों के धुरंधर प्रशंसक, गोलंदाजों के गुण-अवगुण बताने वाले, और विदेशियों की बखिया उधे़ड़ने वाले, सचिन के पक्षधर प्रभाष जी का जाना पत्रकारिता के साथ क्रिकेट का बड़ा नुकसान है।
क्या सचिन को पता है कि उसका एक बड़ा प्रशंसक बौद्धिक दुनिया छोड़ गया?
Thursday, October 1, 2009
बादलों में गुस्ताख़
राम की ड्रेस में सजा कोई बच्चा.. और उसके पीछे दारु पीकर झूमते लोग। रावण का बहुत बड़ा पुतला बनाया हुआ। मेरे शहर के लोगों ने तो इस बार हद ही कर दी थी। उनने रावण के नौ सिर ही लगाए थे। अब उसका फोटो भी है मेरे पास...तो जो राम नहीं कर पाए त्रेता में, वह मेरे तुच्छ शहर के शराबी रामभक्तों ने कर दिखाया।
बहरहाल, आतिशबाजी का पूरा इँतजाम रहा। बांस के ढांचे पर खड़ा राॠम फुलझडियों के छूटने के बीच पटपटाकर जल गया। इस पूरे ठनगन में पंद्रह मिनट भी नहीं लगे। बाकी राॠम को मारने में राम को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, ये कोई राम से ही पूछे।
तो जनाब खलनायक हो तो रावण जैसा..खलनायक का खलनायक और चरित्र में बेदाग..। जो करता रहा सीना ठोंक के, ये ले ये मैंने करा है, तैनूं जो करना है कर ले।
बाद में उसके चरित्र के साथ और भी क्षेपक जोड़ दिए गए। लेकिन रावण जैसे कद्दावर राष्ट्राध्यक्ष को सद्दाम की तरह पंद्रह मिनट में निपटा देना मुझे सुहाया नहीं।
बहरहाल, रावण के प्रति सहानुभूति से भरा मैं मूंगफलियां तोड़ता घर पहुंचा। अगले दिन अल्लसुबह मुझे ट्रेन पकड़नी थी ताकि दिन दो बजे कोलकाता से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ सकूं। कोलकाता पहुंचा तो वहां सड़कों प सन्नटा। लोग दुर्गापूजा की थकान उतारने में लगे थे। फ्लाइट के आसमान में पहुंचते ही मैं भी सातवे आसमान में पहुंच गया, आसमान बादलों से भरा था। मेरी पहले की उड़ानो में ऐसा नही था कि प्लेन ठीक बादलों के बीच से होकर गुजरे।
किताबों में पढ़ा था, कि बादलों के भी कई पर्कार होते हैं। ऐसे में जिन बादलों को मैं ऊपर देख रहा था वह कपासी बादल थे। रुई-से सफेद एकदम झक्क, बुर्राक उजले। इतनी ऊंचाई पर पानी के महीन कण जम जाते हैं और बरफ में तब्दील हो जाते हैं। जाहिर है आसमान में हिलते डुलते भी कम ही हैं। सच कहें तो गोभी के फूलों जैसे आकार वाले बादल... गाना याद आ रहा था आज मैं ऊपर.......।
फिर पता नहीं क्यों मन में स्वर्ग का खयाल आया। सोचा अगर प्लेन अभी क्रैश करता है तो कहां जाऊंगा? मेरी स्वर्ग की यात्रा कैसे होगी। सीधे स्वर्ग (अथवा नरक? मैं खुद को नरक का भागीदार ही मानता हूं, क्योंकि जिन कार्यों में मैं संलिप्त हूं उसे तो धर्म के ठेकेदार पाप कहते हैं। जैसे रावण की प्रशंसा,) बहरहाल, यह तय रहा कि मरा तो शरीर नीचे जाएगा और आत्मा ऊपर जाएगी।
अर्थ यह कि शरीर को नीचे ले जाने से आत्मा का उत्थान होता है। पता नहीं दर्शन क्या कहता है? पहले अगरतला और बाद में गोहाटी को ऊपर से देखा तो लगा कि हमारे देश का यह हिस्सा कितना खूबसूरत है यार। ऊपर से ही मजा आ गया। लगा, किसी ने हरे काग़ज़ को मरोड़ कर रख दिया है और उस पर काई जम गई है। ( अजी हज़रत, एरियल व्यू में पेड़ तो काई जैसे ही दिखेंगे न?)
तो अब कल सुबह में मुझे टीम के साथ डिब्रूगढ़ के लिए कूच करना है और फिर वहां से तेज़ू के लिए तेज़ू म्यांमार और चीन की सरहद के पास है। और लोहित जिले में हैं। सुना है कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी मिस्मी जनजाति की थी, जो लोहित जिले की जनजाति है। यह जानकर तेज़ू मेरा ननिहाल हो गया है, मेरी मां का नाम भी रुक्मिणी ही है।
आगली पोस्ट तेज़ू से..
मंजीत
Thursday, September 17, 2009
बुत हमको कहें काफ़िर....विनोद दुआ बनाम डीडी
पहले तो दूरदर्शन के पचास साल जुमले पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। ठीक है...मान लिया। डीडी में दस हजार गलतियां हैं। चलो ग्यारह हजार होगीं। किस सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सरकारी चैनल बेहूदेपन की हद तक नकारा हैं, आपके साफ-सुथरे और दूध से धुले होने का सार्वभौमिक सत्य स्थापित नहीं हो जाता।
तो जनाब, विनोद दुआ ने डीडी की उम्र ३५ साल कूती। क्योंकि पिछले १५ साल से निजी चैनल मार्केट में उतरे ठहरे। विनोद दुआ जी से कोई पूछे कि आपने अपना करिअर शुरु कहां से किया था? और वह दूरदर्शन छोड़ कर निजी चैनलों में क्यों कूदे? और जब कूदे तो डीडी से क्या ले गए थे? और क्या इसी बहाने वह अपना पिछला हिसाब चुकता तो नहीं कर रहे? और डीडी को ऑटोक्रेटिक ठहराने वाले अपने गिरेबां में झांकेगे क्या?
बहरहाल, सीना तान कर और मूंछों पर ताव देते हुए मैं डीडी का सगर्व दर्शक इसे इसकी पूरी गलतियों के साथ अपनाता हूं। विनोद दुआ के एनडीटीवी की दुकानदारी पूरे सस्ते होने और सड़कछाप हो जाने पर भी नंबर एक नहीं पहुंच पाई है, शायद १५ सितंबर का जेहादी तेवर उसी की परिणति है।
वैसे कूड़ा परोसने में एनडीटीवी भी पीछे नहीं। नेट के झरोखे से, और टीवी के धारावाहिकों औक कॉमिडी शोज़ के अलग से विशेष उनने दिखाने शुरु कर दिए हैं। और हां, १६ सितंबर की शाम विनोद जी का एक और कारनामा दिखा। वैसे एंकर थे तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। रवीश कुमार की फरमाइश पर विनोद दुआ लाइव में उनने फिल्म "उसने कहा था" का एक गीत दिखाया। यहां तक सबकुछ स्वाभाविक था..लेकिन हद तो तब हुई जब सुपर में रवीश कुमार की फरमाइश चलने लगा और एक तस्वीर भी उनकी चस्पां हो गई स्क्रीन पर।
इसी लिए तो हम ग़ुलाम अली के गले की आवाज़ में सुनते हैं .......
"बुत हमको कहें काफ़िर, अल्लाह की मर्जी है.." ...... हैरानी नहीं होती।
दुआ साहब हम मानते हैं कि रवीश आपके आउटपुट हैड हैं, लेकिन,......आप तो डीडी से बेहतर हैं ना?
Wednesday, September 9, 2009
बारिश के बहाने
हमेशा मैंने बरसात को अपने भीतर महसूस किया है। उमड़-घुमड़ कर बरसते बादल आने से पहले ऐसी समां बांधते बस पूछिए मत...ताजी हवा कि गुनगुनती सिहराने वाली खुनक... दरअसल गरमी के बीच थोड़ी भी हवा की ठंडक मजेदार लगती है।
कई बार तो धूल भरी आंधी आती और बादलों के पीछे से झांकते सूरज महाराज की किरणें अजीब माहौल पैदा करती। अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते तो चिल्लाते एक पैसा की लाई बजार में छितराई बरखा उधरे बिलाई... लेकिन कभी बरखा बिला जाती तो कभी हम जैसे नालायकों की दुआ में बिलकुल असर नहीं होता। ताबड़तोड़ बारिश शुरु हो जाती। हम भींगते हुए घर पहुचे नहीं कि मां ने उसी बारिश वाले अंदाज में हमें धोया नहीं।
बरसात होती तो हमारे घर के चारों तरफ जो खाली ज़मीन थी उसमें अरंडी वगैरह के झाड़ उग जाते॥ हमारे खेल के मैदान में घास की हरी चादर बिछ जाती। मैदान के एक किनारे पर पोखरा था, पोखरे में पानी लबालब भर जाता।
एक झाडी़, जिसका नाम पता नहीं उसमे पीले-पीले फूलों को देखकर मन खिल जाता। भटकटैया के फूल चूसते, मीठेपन का अहसास होता। बॉल बिरयिंग की गोलियों जैसे भटकटैया के फल जमा करना हमारे मनोरंजन का साधन होता। बरसात मे हम ड्रैगन फ्लाई पकड़ने उसके पीछे-पीछे घूमा करते। दूब की चादर पर लाल-लाल बीर बहूटियों को पकड़ लेते।
असली मज़ा तो तब आता, जब स्कूल जाने के वक्त जोरदार बारिश हो रही हो, सुबह से ही। माताजी, फिर भी नहीं मानती और छाता लेकर स्कूल के अंदर तक खदेड़ आतीं। बदले में हम वापसी में काले रंग के चमड़े के जूतों में मिट्टी लपेसकर लाल कर आते। गीले जूतों से अगले दिन स्कूल जाने की आशंका प्रायः खत्म हो जाती। लेकिन उसेक बाद घर आते ही जूतों की हालत देखकर माताजी उन्हीं जूतों से हमें दचककर कूटतीं।
हमारे मन में आज भी बरसात का मतलब जमकर बरसना होता है। दिल्ली में तो महज फुहारें होती है। बाद में जब हमने सिगरेट पीना शुरु किया तो चोरी छिपे बारिश होते हुए और अपने दोस्त की प्रेमिका के घर के सामने से भींगते हुए सिगरेट पीने का मज़ा ही कुछ और होता। हां, मीरा के घर के सामने हम सिगरेट को अपने होंठों में ले लेते। ताकि दोस्त की इमेज पर असर न पड़े।
हम लोग कई बार दूर गांव की तरफ निकल जाते थे। झारखंड का ये इलाका हरियाली के लिए मशहूर है, और उस हरियाली को मैं आज भी अपने अंदर जिंदा महसूस करता हूं। हरियाली तो दिल्ली में भी है लेकिन पता नहीं क्यों झारखंड की हरियाली में जो गंध थी, यहां महसूस नहीं हो पाती। झारखंड में इस वक्त पलाश के जंगल में पत्ते आ जाते हैं। और साल के पेड़ की हरियाली में अलग-अलग शेड्स आ जाते हैं।
तो बरसात के इन्हीं दिनों कई बार ओले भी पड़ते। कई बार तो ओले की बौछारों से सड़क कि किनारे और घास सफेद लगने लगा जाता। कहावत थी कि ओले खाने चाहिए फायदा होता है। उस फायदे की आड़ में हम खूब बऱफ के टुकड़े चुनते फिरते।
दिल्ली में ओले गिरे भी तो हम कभी चुनकर खा नहीं पाए। कभी सम्मान के नाम पर..कभी बड़ा हो गया हूं यह सोच कर। बारिश के नाम पर रोमांस के टुकड़े तो हमने खूब देखे, लेकिन कभी यह सोचा है कि बारिश में आसमान के आंसू गिरते हैं।?
अरे हां, याद आया। एक बार उड़ीसा में महाचक्रवात आया था.. शायद ९७ में। हमारे शहर में सात दिनों तक लगातार बारिश होती रही। पहले दो दिन तो मजा आया, लेकिन बाद में लगातार बिजली गुल रहने, बाहर दोस्तों से नहीं मिल पाने और कई दूसरी वजह से बारिश बोझ लगने लग गई।
फिर भी, बारिश अपने चंद्रमुखी स्वरुप में बेहतर होती है। वह ज्वालामुखी न बने तो ही बेहतर।
Friday, September 4, 2009
अमिताभ के जूते में शाहरुख के पांव

1970 की शुरुआत से लेकर 1990 तक अमिताभ एक एंग्री यंगमैन का प्रतिरूप बन गए थे, जो अपन बाग़ी तेवरो से नौजवान भारत की आवाज़ था। लेकिन अमिताभ बच्चन के बाद 90 के दशक में फिर से भारत बदला, नई नीतियां आ गईं और विकास की ओर जाने के रास्ते बदले, तो बाग़ी तेवरों के ग़ुस्से में दर्शकों के लिए जो अपील थी, वो ख़त्म होने लगी।
एक क़िस्म का जो रेगुलराइजेशन, वैश्वीकरण होने लगा, रोज़गार के नए मौके आए, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में जो हो रहा था उसे दिखाने के लिए सिनेमा में नए चेहरों की ज़रुरत पड़ी। तो फ़िल्मों में जो तीन खा़न हैं शाह रुख़, सलमान और आमिर ख़ान का आना शुरु हो गया।
एंग्री यंगमैन के अमिताभ के चरित्र को शाहरुख ख़ान ने थाम लिया। वे आज के वैश्विक भारतीय के चरित्र को जीते हैं, हैं जो कि हर स्थिति में बेहतर है। इसे नौकरी के लिए कतार में लगना नहीं होता, उसे भूख की चिंता नहीं है वह एनआरआई है, और एनआरआआई के मनोरंजन का सरंजाम जुटाता है।
वो विश्व में कहीं भी काम कर सकता है, उस क़िस्म का जो नया आशावादी, सकारात्मक चरित्र जो है और डेविल में केयर एटीट्यूड भी है। पर वो साथ ही साथ बहुत होशियार भी है। 90 के दशक से शुरु होकर यह अभी तक चले जा रहा है।
तीनों ख़ानो में सलमान अगली कतार के दर्शकों के हीरो है तो शाह रुख़ और आमिर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ परोस रहे हैं। उन में आमिर का अंदाज़ कुछ ज़्यादा बेहतर है।
शाह रुख़ खान के पीछे युवा वर्ग इस तरह दीवाना है जैसे कभी राजेश खन्ना और देवांनंद के करिश्मे से रोमांचित था।
आमिर में शाह रुख़ जैसी अपील तो नही है लेकिन वह अदाकारी में शाह रुख़ से कई क़दम आगे हैं। शाह रुख़ तड़क-भड़क में आगे हैं लेकिन अपनी फ़िल्मों में मैथड एक्टिंग के ज़रिए आमिर, शाह रुख़ के जादू पर काबू पा लेते हैं।
लगान हो या तारे ज़मीं पर, आमिर ने अपनी काबिलियत साबित की है। एक तरह से आमिर मिडिल सिनेमा में मील के पत्थर है तो शाहरुख सुपर सितारे की परंपरा के वाहक। और यही आज के युवा का मूलमंत्र भी है। इधर, शाह रुख़ के आमिताभ के हर जूते में पैर देने की सनक सवार है। अमिताभ की शहंशाह की उपाधि के बरअक्स वह बादशाह कहलाना पसंद करते हैं। (ये बात और है कि शहंशाह और बादशाह दोनों ही, निहायत ही वाहियात और सुपर फ़्लॉप फ़िल्मे ठहरी हैं) ।
कौन बनेगा करोड़पति से लेकर डॉन और ऐसे ही कारनामे शाह रुख कर रहे हैं, जिससे वह खुद को अमिताभ या उससे ऊपर कहलना पसंद करते हैं। यह उनकी निजी आकांक्षा हो सकती है, लेकिन पहले भी हमने बात की थी कि अभिनेता का निजी भी सार्वजनिक होता है, तो इस तरह से जनता में कोई खास बढिया संदेश तो नहीं जा रहा।
मंजीत ठाकुर
Monday, August 31, 2009
डेडिकेटेड टू माइ फर्स्ट लव
किताब जेपी पर थी, गंभीर और बेहतरीन थी। लेकिन ये डेडिकैशन सबसे ज्यादा संजीदा लगा। लोग अपने पहले प्रेम को नहीं भूल पाते हैं क्या? वैसे, मैंने तभी तय कर लिया कि अपनी किताब (अगर कभी लिखी गई) तो पहले पन्ने पर मैं भी ऐसी ही लाईनें लिखूंगा...डेडिकेटेड टू माई फर्स्ट लव..। कोई नाम नहीं दूंगा कि यह किताब मेरी प्रेयसी मुन्नी, चुन्नी गुड़िया, चीकू, बन्नी, बिट्टी, गुड्डी या मिली को समर्पित है।
नाम लेने का मतलब संभावनाओं का अंत, तुरंत..।
इससे होगा क्या कि आपकी मौजूदा लव को लगेगा कि यह किताब उन्हीं के लिए है और आपके बिना सुबूत दिए यह साबित हो जाएगा कि आपका पहला प्यार वही है।
दूसरे, आपके पहले, दूसरे, तीसरे...और जितने भी आपकी औकात के हिसाब से प्यार हुए हों, हरेक को लगेगा कि किताब उन्हीं को समर्पण है। कई लोग राजेंद्र यादव, तो कोई नामवर सिंह को समर्पित करते हैं। हम उनको करेगे जिनसे हमारा मतलब सध चुका है और भविष्य में कभी संभावना होगी कि पुनः सधेगा।
विद्वज्जन कहते हैं लव चाहे किसी भी नंबर पर क्यों न आए होता हमेशा फर्स्ट ही है। वैसे ही जैसे मुनियों ने कंस को मिसगाइड किया था कि आपकी बहन के आठवें गर्भ की संतान आपका नाश करेगी.. आठवें गर्भ को लेकर चक्कर चल गया था। कंस परेशान था लेकिन आपको ऐसी परेशानी पेश नहीं आनी चाहिए..।
दरअसल, ऐसे समर्पण से यह साबित हो जाएगा कि आप कितने समर्पित प्रेमी रहे हैं। और एक साथ कईयों से उत्कट समर्पण का ऐसा लाजवाब आईडिए को पेंटेंट करवाने जा रहा हूं।
हर मर्ज की दवा है गुस्ताख के पास। लेकिन मैं किसी को गिनी पिग नहीं बनाने जा रहा हूं । पहला प्रयोग मैं खुद करुंगा। खुद पर। आप चाहें तो मेरे फॉर्म्युले का इस्तेमाल कर सकते हैं..। बाइलाइन देने का कोई चक्कर नहीं, हां नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा( बतर्ज-गांधी शांति प्रतिष्ठान की किताबें)
तो गुस्ताख़ का यह आइडिया कैसा लगा आपको? है ना दूर की कौड़ी?
Thursday, August 27, 2009
गुस्सैल नौजवान अब फेंके हुए पैसे भी उठाता है- बदलता दौर बदलते नायक

उन्ही दिनों परदे पर रोमांस की नाकाम कोशिशों के बाद एक बाग़ी तेवर की धमक दिखीी, जिसे लोगों ने अमिताभ बच्चन के नाम से जाना। गुस्सैल निगाहों को बेचैन हाव-भाव और संजीदा-विद्रोही आवाज़ ने नई देहभाषा दी। और उस वक्त जब देश जमाखोरी, कालाबाज़ारी और ठेकेदारों-साहूकारों के गठजोड़ तले पिस रहा था, बच्चन ने जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के ज़रिए नौजवानों के गुस्से को परदे पर साकार कर दिया।
विजय, के नाम से जाना जाने वाला यह शख्स, एक ऐसा नौजवान था,ा जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, और जिसको न्याय नहीं मिले तो वह अकेला मैदान में कूद पड़ता हैै।
लेकिन बदलते वक्त के साथ इस नौजवान के चरित्र में भी बदलाव आया। जंजीर में उसूलों के लिए सब-इंसपेक्टर की नौकरी छोड़ देने वाला नौजवान देव तक अधेड़ हो जाता है। जंजीर में उस सब-इंस्पेक्टर को जो दोस्त मिलता है वह भी ग़ज़ब का। उसके लिए यारी, ईमान की तरह होती है.
लेकिन उम्र में आया बदलाव उसूलों में भी बदलाव का सबब बन गया। देव में इसी नौजवान के पुलिस कमिश्नर बनते ही उसूल बदल जाते हैं, और वह समझौतावदी हो जाता है।
लेकिन अमिताभ जैसे अभिनेता के लिए, भारतीय समाज में यह दो अलग-अलग तस्वीरों की तरह नहीं दिखतीं। दोनों एक दूसरे में इतनी घुलमिल गए हैं कि अभिनेता और व्यक्ति अमिताभ एक से ही दिखते हैं। जब अभिनेता अमिताभ कुछ कर गुज़रता है तो लोगों को वास्तविक जीवन का अमिताभ याद रहता है और जब असल का अमिताभ कुछ करता है तो पर्दे का उसका चरित्र सामने दिखता है।
अमिताभ का चरित्र बाज़ार के साथ जिस तरह बदला है वह भी अपने आपमें एक चौंकाने वाला परिवर्तन है। जब ‘दीवार’ के एक बच्चे ने कहा कि उसे फेंककर दिए हुए पैसे मंज़ूर नहीं तो लोगों ने ख़ूब तालियाँ बजाईं।
बहुत से लोगों को लगा कि यही तो आत्मसम्मान के साथ जीना है। उसी अमिताभ को बाज़ार ने किस तरह बदला कि वह अभिनेता जिसके क़द के सामने कभी बड़ा पर्दा छोटा दिखता था, उसने छोटे पर्दे पर आना मंजूर कर लिया।
फिर उसी अमिताभ ने लोगों के सामने पैसे फ़ेंक-फेंककर कहा, ‘लो, करोड़पति हो जाओ.’ कुछ लोगों को यह अमिताभ अखर रहा था लेकिन ज्यादातर लोगों को बाज़ार का खड़ा किया हुआ यह अमिताभ भी भा गया।
बहरहाल, अमिताभ आज भी चरित्र निभा रहे हैं, लेकिन उनके शहंशाहत को किसी बादशाह की चुनौती झेलनी पड़ रही है। हां, ये बात और है कि शहंशाह बूढा ज़रुर हो गया है पर चूका नहीं है। बाज़ार अब भी उसे भाव दे रहा है क्योंकि उसमें अब भी दम है।
Monday, August 24, 2009
बदलता दौर, बदलते नायक-३

दिलीप-देवानंद और राज कपूर के दौर के ठीक बाद या उसके दौरान ही हिंदी सिनेमा में सुपरस्टारडम की शुरुआत हुई। इस दौर में राजेश खन्ना रौमांटिक किरदारों में नजर आते रहे। वे दिलीप कुमार की परंपरा में थे। किशोर कुमार की आवाज़ गीतों के लिए परदे पर राजेश खन्ना की आवाज़ बन गई। राजेश खन्ना दरअसल एक मैटिनी आइडल थे।
बाद अपने जमाने के टॉप आइडल राजेश खन्ना के लिए जनता के बीच एक खास क़िस्म का हिस्टिरिया था।
लेकिन उनके ज़माने तक समाज में बहुत कुछ बदल रहा था। सिनेमाई परदे पर पेड़ों के इर्द-गिर्द नाच-गाने लोगों को पसंद तो आ रहे थे और दुनियावी मुश्किलों को लोग कुछ देर के लिए भूल तो जाते लेकिन यह महज इसलिए था क्योंकि दर्शक के पास विकल्प नहीं थे।
मुख्यधारा के सिनेमा में विकल्प नहीं थे और दर्शक अभी तक गंभीर कला सिनेमा को झलने के मूड में नहीं था। ऐसे में कुरते और पैंट का काकटेल चलता रहा.. किशोर कुमार की आवाज़ में गाने बजते रहे, फिल्में हिट होती रहीं लेकिन इनमे समाज का सच नहीं था।
राजेश खन्ना के कुरते और पैंट के कॉकटेल की भी कहानी है, खासकर उनके शर्ट को बाहर रखने की भी। उनकी कमर ज्यादा फैली हुई थी, तो उसे ढंकने के लिए शर्ट बाहर रखना ज़रुरी था। राजेश खन्ना के गरदन को अदा से हिलाना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। रोमांस के बाद०शाह बन चुके खन्ना पेड़ों के इर्द-गिर्द ही दौड़-दौड़ कर नायिकाओं के आगे पीछे गाने गाते रहे। हां, आनंद जैसी कुछ फिल्में ज़रुर बेहतर थीं, लेकिन इनमें निर्देशक की कुशलता अधिक नायक की अपनी छवि कम थी। जाहिर है, सिनेमा का एक बेहद प्रचलित मुहावरा विलिंग सस्पेंसन ऑफ़ डिसविलिफ़ सच होता दिख रहा था।
लेकिन तब राजेश खन्ना के इस सुनहरे सपनों वाले हवाई किले को तोड़ने वाली एक बुलंद शख्सियत की ज़रुरत थी। और ये शख्सियत सिनेमा में दस्तक दे चुकी थी।
Saturday, August 22, 2009
कविता- पोशीदा रंग
Friday, August 21, 2009
बदलता दौर, बदलते नायक-२

दरअसल, रचनाशीलता के बारें में हमारे गुरु बलराम तिवारी कहा करते थे कि जभ तक आपके विचार आपके मन में हैं, वह आपकी निजी संपत्ति हैं, लेकिन काग़ज़ पर उतरते ही अभिव्यक्तियां सार्वजनिक संपत्ति हो जाती हैं। गुरुदत्त की रचनाओं के बारे में, जो काग़ज़ पर भी थी और सिल्वर ब्रोमाइड से रंगी प्लास्टिक पर भी, यही कहा जा सकता है।
गुरुदत्त ने परदे पर एकत अलग तरीके के नायक की रचना की। भावुकता में करीब-करीब शरतचंद्रीय बाना लिए इसनायक पर दुखों का पहाड़ था। काग़ज़ के फूल की बात करें तो इस नायक ने दुनिया के बेगानेपन पर अपनी तल्ख़ टिप्पणी छोड़ी। और जहां तक निजी अभिव्यक्तियों की बात है, वहीदा उनकी फिल्मों का मुख्य स्वर बनकर उभरी। गुरुदत्त की फिल्मों में परदे पर वहदा के बेहतरीन क्लोज शॉट्स इस बात की तस्दीक करते हैं।
दो बीघा ज़मीन की बात करें, तो उस ज़माने की यह पहली फिल्म थी, जिसमें इटालियन नव-यथार्थवाद की झलक तो थी ही, इसका कारोबार भी उम्दाा रहा था। फिल्म वायसिकिल थीव्स से एक हद तक प्रेरित थी और रचनाशीलता के स्तर पर भी कलात्मस विचारधारा झलक रही थी।
फिल्म में बलराज साहनी थे, बेदखल सीमांत किसान की भूमिका को बलराज ने जीवंत कर दिया था। वह ज्यादा आश्चर्यजनक इसलिए भी था क्योंकि उन्हीं दिनों देव-दिलीप और राज कपूर परदे पर रोमांस ही उकेर रहे थे।
हालांकि, दिलीप कुमार ने आवाज़ के मामले में अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया, और ज्यादातर अँडरप्ले कर अदाकारी की। फिर भी, असल जिंदगी में बेहद अभिजात्य बलराज साहनी ने गरीबी को परदे पर जी दिया।
इसी दशक में मदर इंडिया भी आई। परदे पर विद्रोह दिखा। महबूब ख़ान ने जो दिखाया, उसमें भी आदर्शवाद था। नरगिस ने मां को उकेरा...भारत माता के रुप में। अपने ही डकैत बेटे को गोली मारकर इस मदर इंडीया ने आदर्शवाद की नई छवि गढ़ दी। लेकिन दर्शकों का एक ऐसा वर्ग तैयार होना शुरु हो चुका था, जिसकी सहानुभूति डकैत बेटे सुनील दत्त से थी।
लेकिन, साठ के दशक में भी फिल्मों में नायक आते तो रहे लेकिन उनका स्वरुप कमोबेश वैसा ही रहा। पेड़ों के इर्द-गिर्द घूमकर गानेवाले हीरो की। साठ के दशक में लेकिन बदलाव की रुपरेखा तैयार होनी शुरु हो गई थी। मुग़ल-ए-आज़म ने दिलीप कुमार को ट्रैजिक रोमांस के शिखर पर बैठा दिया। लेकिन इसी दशक में एक देशभक्त नायक का आविर्भाव भी हुआ। उपकार में मनोज कुमार ने देशभक्ति को एक नया एंगल दिया और जल्दी ही भारत कुमार बन बैठे।
संगम ने विदेशों में शूटिंग करने का ट्रेंड शुर कर दिया। लेकिन बॉलिवुडीय नायक कुछेक अपवादो ंको छोड़ दें तो रोमांस की परिक्रमा ही करता रहा। 1969 को शक्ति सामंत की ब्लॉकबस्टर आराधना ने रोमांस के एक नए महानायक को जन्म दिया। जो पूढ रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू....
Monday, August 17, 2009
बदलता भारत, बदलते नायक-1
 सन 47 में जब देश आजा़द हुआ, तो उस समय एक नया जोश था, अपनी आजादी और भविष्य को लेकर। कैसा भविष्य हिंदुस्तान को चाहिए, ये आदर्शवाद फिल्मों में भी दिख रहा था। उस जमाने में जो भी फिल्म बनती थीं उनके चरित्रों में उस वक्त की जिंदगी की झलक साफ दिखाई देती थी।
सन 47 में जब देश आजा़द हुआ, तो उस समय एक नया जोश था, अपनी आजादी और भविष्य को लेकर। कैसा भविष्य हिंदुस्तान को चाहिए, ये आदर्शवाद फिल्मों में भी दिख रहा था। उस जमाने में जो भी फिल्म बनती थीं उनके चरित्रों में उस वक्त की जिंदगी की झलक साफ दिखाई देती थी।
इसी दौरान सिनेमाई परदे पर देवानंद, राजकपूर और दिलीप कुमार सितारे की तरह उगे। लंबे समय तक भारतीय सिनेमा का दर्शक इन तीनों अभिनेताओं में अपने को और अपने आसपास को तलाशने की कोशिश करता रहा।
इस तिकड़ी में दिलीप कुमार असल में रोमांटिक रोल करते थे और दिलीप कुमारनुमा रोमांस का मतलब था ट्रैजिक रोमांस। दिलीप कुमार, रोमांस हो या भक्ति, मूल रुप से अपनी अदाकारी को केंद्र में रखते थे। एक ट्रैजिक हीरो के रुप में उनकी पहचान बन गई थी और वे ट्रेजिडी किंग के नाम से मशहूर भी हो गए।
आजादी के बाद के युवाओं में रोमांस का पुट भरा, देवानंद ने। देवानंद कॉलेज के लड़कों में, एडोलेसेंट लेवल पर काफी लोकप्रिय थे। खासतौर पर शहरों के युवा वर्ग में उनकी गजब की पकड़ थी।
राज कपूर का मामला इन दोनों से अलग था। वे एक अच्छे अभिनेता तो थे ही लेकिन अभिनेता से भी बड़े निर्देशक थे। अपनी फिल्मों में अदाकार के तौर पर उन्होंने हमेशा आम आदमी को उभारने की कोशिश की। एक सामान्य आदमी को गढ़ने में उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा लगा दी। आर के लक्ष्मण के आम आदमी की तरह के चरित्र उन्होने रुपहले परदे पर साकार करने की कोशिश की।
एक आम आदमी, किस तरह देश और समाज के भीतर के बदलावों को समझता है, कैसे इस दुनिया को देखता है, उस किस्म के किरदार उन्होंने करने शुरु किए। 10-12 सालों तक उन्होंने इसी तरह की फिल्में बनाईं। ऐसी ही फिल्मों के सहारे वे एक अभिनेता के साथ-साथ एक मंझे हुए निर्देशक के रुप में उभर कर सामने आए।
राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, इन तीनों का एक खास स्टाइल था। वह स्टाइल अब भी एकतरह से कायम ही है, क्योंकि हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए ये तीनों एक स्टाइल आइकॉन थे।
पहले हम देखें तो देवानंद और दिलीप कुमार की अदाकारी का वही सिलसिला चला जिसके लिए वो मशहूर थे। लेकिन राज कपूर ने कुछ- कुछ जगहों पर खुद को बदला भी, वो एक आम आदमी बन गए जिसमें चार्ली चैपलिन किस्म का चरित्र भी उन्होंने कई तरीकों से दिखाया।
लेकिन इन तीनों का जादू तब चुकने लगा...जब एक किस्म का रियैलिटी चेक (जांच) जिदंगी में आया। परदे पर जो दृश्य बन रहा था, उसका धरातल से कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था। ऐसे में इनकी अदाकारी चलती तो रही लेकिन उसमें वो दीवाना कर देने वाली अपील बची नहीं रही, जिसके लिए लिए तीनों मशहूर थे।
Saturday, August 15, 2009
ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के
पहले देश को, देशवासियों को, ब्लॉग जगत के लिक्खाडों को ज़श्ने-आजादी की मुबारकवाद, मुबारकबाद उन्हें जो आम हैं, खास नहीं। और ऐसे ही रहे ईमानदार वगैरह तो जिंदगी भर आम ही रहेगे। लेकिन असली अभिनंदन, उन भ्रष्टाचारियों का जो देश को बपौती का माल समझकर दीमक का अनुसरण किया करते हैं।
हे बेईमानी के मील के पत्थरों, आजादी की इस सालगिरह पर उन तमाम लोगों के दिलों पर गिरह लग गई होगी, जिन्होंने पता नहीं क्या सोचकर खून-पसीना वगैरह बहाकर, अंग्रेजो की गोलियां वगैरह खाई। तुम लोगों के गुरदे, जिगर दिल बेचो, शर्म और हया के साथ ईमान बेचो...स्वाईन फ्लू से बचाने वाले मास्क से लेकर दवा तक कालाबाजार के हवाले कर दो, खरीदने वालों की होगी औकात तो खरीदेंगे वरना न तो देश में लकडियों की कमी है ना कब्र के लिए ज़मीन की।
ट्रेन में बिना टिकट चलने वाले हे महासपूतों, टिकट लेकर चलना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पर..। एक अदने से टिकट चेकर की यह औकात कि तुम जैसे वीर को टिकट लेने पर मजबूर करो। देश की हर रेल पर तुम्हारा अधिकार है। हर गाड़ी तुम्हारे ही पूज्य पिता की है, जब चाहों आंदोलन के नाम पर इसे फूंक दो।
और, हे उन पिताओं का सच्चे सपूतों, सुबह उठकर अपने मलमूत्र वगैरह सड़क के किनारे ही सादर समर्पित करो। इससे बरसात के इस मौसम में क्या ही मनोरम छटा पैदा होती है.. हरी-हरी घास पर पीला-पीला गू... मानो हरी चादर पर सुनहरे बेलबूटे...।
दाल, चावल आटा, गन्ना, चीनी, पेट्रोल. जो इच्छा हो जिस चीज़ की इच्छा हो, ब्लैक में बेचो। काला धन, धन के नस्लवाद को कम करता है, धन के रंग भेद के खिलाफ फतवा है।
हे आम आदमी, तुम चक्की में पिसने वाले घुन हो, तुम बलियूप की प्रतीक्षा में खड़े पाठा अर्थात् मेमने हो, तुम दड़बे में दुबक कर अपनी मौत का इंतजार कर रहे मुर्गी के नपुंसक संतान अर्थात् चिकन हो.. लेकिन यह भरोसा रखो कि तुम्हारे नेता भी तुम्हारी तरह हैं। ....ये बात और है कि कुछ लोग उन चिकनों को हेडलैस चिकन कह जाते हैं......उनका भरोसा करो.. वह भरोसा तो दिला ही रहे हैं और मंहगाई बढेगी, दाल-चीनी मंहगी होगी. मौत के दिन नजदीक आंगे..पानी कम बरसेगा...माटी और गरम होगी।
हे आम आदमी अगर तुम रैकेट नहीं चला सकते, ध्रुव के निकट नहीं जा सकते.. तो आम तो नहीं ही रहोगे अमरुद और शरीफे भी नहीं बन पाओगे।
अतः हे कापुरुषों अगर भ्रष्टाचार के अतिचार के संवाहक अर्थात् वैक्टर बनकर इस परंपरा के अंग नहीं बन सकते तो अपने अंग भंग के लिए तैयार रहो।
अतएव आजादी के इस पावन दिवस पर गुस्ताख की सीख मानो और िस गीत को गुनगुनाओ
'घोटालों की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के...
ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। '
आमीन।
Wednesday, August 12, 2009
रहमान अनप्लग्डः पर श्रोता निराश

दूरदर्शन के पचास साल इसी १५ सितंबर को पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। सो, कल यानी ११ अगस्त से एक कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हुई है और सही ही इसका उद्घाटन कार्यक्रम रहमान साहब के कार्यक्रम से हुआ।
बहरहाल, रहमान अनप्लग्ड की शुरुआत बेहतर रही।
फिर आए शिवमणि. और इस ड्रमर ने पहले जालियां और सूटकेस बजाया। शिवमणि को बहुत दिनों से देखता आ रहा हूं लेकिन उनकी हर प्रस्तुति पहले से अलग होती है। शिवमणि के ड्रम को सुनना अद्भुत है। उंगलियां ही सुमिरनी बना ली हैं मणि ने। मणि तो सचमुच मणि हैं भारत मां की ताज के ।
फिर आए हरिहरन...तू ही रे.. से शुरु किया। सूदिंग कहते हैं ना जिसे अंग्रेजी में, उनकी आवाज़ से कुछ वैसा ही लगता है। मखमली.. या कहें शहद टपकती-सी आवाज़। कैलाश खेर की आवाज़ मे अगर पहाड़ी नदी सी चंचलता और जलप्रपात सी ऊंचाई है तो हरिहरन की आवाज में वह नदी मैदानी हिस्से में कलकल करती बहती लगी। गहराई और वॉल्यूम के लिहाज से भी।
आखिर में, हरिहरन ने रोजा का भारत हमको जान से प्यारा है गाया। साधना सरगम ने किसना फिल्म का भजन गुगुनाया ..बस हो गया खत्म। रहमान पता नहीं क्यों गाने स्टेज पर नहीं आए। जय हो..तो जाने दीजिए वंदे मातरम् भी नहीं गाया। हम इंतजार करते रहे। वैसे रहमान कंसर्ट के दौरान पियानो बजाते रहे लेकिन हम तो उनकी जादुई आवाज़ सुनने के लिए बेताब थे।
बड़ी निराशा हुई। वह निराशा अभी तक तारी है। वैसे रात में हम घर गए १२ बजे के आसपास तो वंदे मातरम प्लेयर पर चला कर सुन ज़रुर लिया, लेकिन निराशा कम नहीं हुई। वो इसलिए कि रहमान की आवाज़ में लाइव सुनना अलग मज़ा देता और हम रहमान के प्रशंसकों में से एक हैं।
चलिए फिर कभी सही..।
Wednesday, August 5, 2009
सफ़रनामा- इंसेफेलाइटिस के इलाके में

बनारस के बाद हमने जी टी रोड अर्थात् एनएच-२ का दामन छोड़ दिया। गरमी और उमस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, जो हमें महसूस हो रहा था, वह सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। उसे बताया नहीं जा सकता है।
गाजीपुर शहर से बाहर निकलते वक्त एक दुकान पर हमने पकौडियां खाईं और जलेबी भी। चाय इतनी शानदार थी.. उसमें अब बिहार की मिट्टी का सोंधापन आने लगा था।
आज़मगढ़ पहुंचे तो एक नई स्टोरी हमारा इंतजार कर रही थी। आज़मगढ़ के गांवो में नई पीढी के लोग नहीं मिलते और आज़मगढ़ को जिस वजह से बदनाम किया जाता है उसका भी कोई निशां हमें दिखा नहीं।
आजमगढ़ की समस्या है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। क्या हिंदू क्या मुस्लिम..हर संप्रदाय के लोग रोज़गार के लिए इलाका छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बदनामी है जिसकी वजह से नौकरी मिलती नहीं बाहर..। बनारस के बाद गोरखपुर तक हमें सारनाथ, सैदपुर, गाज़ीपुर, बिरनोन, मरदा, मऊनाथभंजन, घोसी, दोहरीघाट और चिल्लीपुर वगैरह पार करना पड़ा।
जहां तक मुझे याद है दोहरीघाट के पास हमारे कैमरामैन गंगा-गंगा करते शूट करने कार से उतर पड़े। लेकिन वह घाघरा नदी थी। पानी एक दम साफ। सुनील नहाने के मूड में आ गया और हमारा ड्राइवर भी। लेकिन मुझे लगा कि स्वाति के सामने नहाना.. ठीक नहीं रहेगा। कोई सिक्स पैक-वैक तो है नही हमारे पास। तो बेवजह अपने स्वास्थ्य पर तीखी टिप्पणियां क्यो सुनी जाए? आ बैल (गाय) मुझे मार वाले स्टाइल में।
बहरहाल, गोरखपुर के बारे में हमने सुन रखा था कि यहा जापानी बुखार का बड़ा कहर है। और हजारो बच्चों की जान हर साल चली जाती है।
गोरखपुर पहुंचे तो वहां के डॉक्टर आर एन सिंह से हमारी मुलाकात हुई। सिंह साहब ने इँसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। गोरखपुर की हालत ये है कि वहां २००५ में ४ हजा़र से ज्यादा २००६ में करीब ५ हजार २००७ में साढे चार हजार और २००८ में दो हजार बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। केंद्र ने टीकाकरण का काम किया है लेकिन एक बार टीकाकरण के बाद कर्तव्यों की इतिश्री मान ली गई। सूअर पालन पर कोई रोक वोट की वजह से नहीं लगाया जा रहा है।
क्या बिडंबना है..। अमीरो की बीमारी स्वाईन फ़्लू पर केंद्र का रुख देखिए और गरीबो और पूर्वांचल की बीमारी इंसेपेलाइटिस पर सरकार का रवैया..। स्वाइन फ्लू से अब तक मेरी अद्यतन और अधिकतम जानकारी से महज एक लड़की की मौत हुई है- पुणे में। कोई शुबहा नहीं, एक भी मत नहीं होनी चाहिए और स्वाइन फ्लू की रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन इँसेफेलाइटिस पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रुरत है और अभी क्या ताजा़ आंकडा़ है बीमारों का इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स की तचरफ से भी अभी तक कोई फॉलो-अप नहीं है।
इँसेफेलाइटिस पानी से होने वाला रोग है। सूअर इसका वैक्टर है। ड़ॉ सिंह ने इसेक लिए ेक सस्ता उपाय हमें बताया। साफ बाल्टी में पानी को रख कर उसे कपड़े से ढंक दें और सूरज की रौशनी में २ घंटे छोड़ दें..इसमें इँसेफेलाइटिस के वायरस मर जाते हैं। इससे उबालने का खर्च भी नहीं।
ऊपर जो आंकड़े मैंने दिए हैं वह नजदीकी अंको तक साधे गए हैं और सरकारी अस्पतालों के हैं। असल आंकड़ा इसेस ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर साहब के यहां से निकले तो चार बज गए थे शाम के। मेरी मंजिल थी बेतिया। जहां गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम मुन्ना ने किया था। मुन्ना डीडी के स्ट्रिंगर हैं बेतिया में और असरदार काम करते हैं। लेकिन गोरखपुर से आगे का हाल अगली पोस्ट में।
जारी...
Tuesday, August 4, 2009
जिंदगी की आवाज़ थे किशोर दा
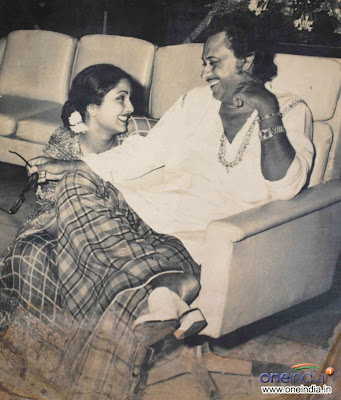
मेरी पीढी़ की तरफ से किशोर दा के हुनर को प्रणाम..।
Sunday, July 26, 2009
लमही में
बजट यात्रा के दौरान इस बात का मौका मिला कि लमही जाऊं। कबीर साहब के गांव से निकलते ही मैंने राजीव (ड्राइवर ) को कहा सीधे लमही चलने के लिए। राजमार्ग पर ही एक बड़ा से गेट बना है, मुंशी प्रेमचंद स्मारक गेट। उसके साथ ही दसफुटिया पक्की सड़क आपको लमही तक ले जाएगी।
पूरे गांव की सड़के साफ-सुथरी थी। नरेगा के ज़रिए ठीक काम हो रहा था। नालियां भी साफ थी। एक आम भारतीय गांव से थोड़ा अलग लगा लमही। कम से कम पहली नज़र में ..। गांव में कई भारत मार्का हैंडपंप लगे थे। खेत में फसल भी थी ठीक ही थी। शायद मूंग थी।
Wednesday, July 22, 2009
सूर्यग्रहण और मेरा तजुर्बा
स्कूल की इमारत की सबसे ऊपरवाली छत पर हम अपने कैमरे लिए तैनात थे। सुबह चार बजे से ही कि ज्यों ही सूरज उस्ताद दिखे, कैमरे में क़ैद कर लें। लेकिन बरसात ने पानी फेर दिया। फिर भी तजुर्बा बेहतरीन रहा। ६ बज के ४ मिनट पर सूरज को तयशुदा वक्त पर ड्यूटी पर आना था। वह आए भी। लेकिन ६.२१ पर राह में राहु के किरदार में चांद की एंट्री होनी थी। हो गई। कुदरत में ऐसी चीजें डायरेक्टर के कंट्रोल से बाहर नहीं जातीं। ये कोई नीरज वोरी की फिल्म शार्टकट-द क़ॉन इज़ ऑन तो थी नहीं कि चीजें निर्देशक के हाथ से बाहर हो जाए और पिट जाए फिल्म। बहरहाल, नायक और खलनायक तय थे। बाद में इंद्र देवता खलनायक के रुप में जगजाहिर हुए।
बच्चों ने मोमबच्ची जला कर सूरज को नमस्कार किया था। वह अंधेरा छाते ही केंडल लाईट ब्रेकफास्ट करने लगे। इसका इंतजामन स्कूल में किया गया था ताकि ग्रहण के दौरान न खाने के मिथक को तोड़ा जा सके। हालांकि सूरज को न देख पाने का मलाल सबको था लेकिन इसे एक हद तक हमारी टीम ने इंतजाम किया था। एक टीवी पर हमने अलग अलग जगहों में ग्रहण के लाइव दिखाने की व्यवस्था की थी। बच्चों ने इसे देककर संतोष कर लिया।
वैसे एक बात और पता लगी कि सूर्यग्रहण में पहले सूर्य का कोरोना भी नहीं दिखता था और पूरी तरह अंधेरा छा जाता था क्योंकि चांद धरती के ज्यादा पास था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि धरती की परिक्रम करने वाली चांद की कक्षा हरेक साल ३.५ सेटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अगले ६०० मिलियन साल के बाद चांद इतनी दूर हो जाएगा कि धरती पर पूर्ण सूर्य ग्रहण मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसकी कक्षा २३,५०० किलोमीटर ज्यादा बड़ी हो जाएगी।
वैसे बता दें कि पूर्ण सूर्यग्रहण तभी मुमकिन हो पाता है जब धरती सूर्य की ओर चक्कर लगामे वाले अपने अंडाकार रास्ते में सूर्य से सबसे दूर हो (एपहेलियन) और इसी वक्त चांद अपने अंडाकार रास्ते में धरती के सबसे नज़दीक हो (पेरिजी)। इसके साथ ही धरती और सूर्य के बीच चांद एक सीध में आ जाए..यही स्थिति पूर्ण सूर्यग्रहण पैदा करती है और दुर्लभ भी मानी जाती है।
अब अगली बार, २१३२ इस्वी में जब अगवा पूर्ण सूर्यग्रहण लगेगा तो मैं हवाई जहाज से देखूंगा. अगर आप इच्छुक हैं तो बता दो, अभी एक पर एक फ्री टिकट मिल रहा है मुझे।
Monday, July 20, 2009
कबीर के गांव में-२
 हम जब कबीर के गांव पहुंचे, तो हवा में अजब-सी आध्यात्मिकता घुली थी। १० फीट चौड़ी सड़क पक्की थी। लेकिन सड़कों के पक्का होना गांव की तरक्की का सुबूत नहीं थी। गांव में पक्के मकान थे, लेकिन कुछेक ही। गांव के प्रधान का मोबाईल नंबर हमारे पास था। बनारस में ही एक जानकार से मिल गया था। लेकिन लहरतारा के पास ही कटवां गांव.. लहरतारा वहां से तीन किलोमीटर दूर है। हां के निवासियों ने बताया कि प्रधानजी के पास जाएंगे तो वह सच का सामना क्योंकर करवाने लगे?
हम जब कबीर के गांव पहुंचे, तो हवा में अजब-सी आध्यात्मिकता घुली थी। १० फीट चौड़ी सड़क पक्की थी। लेकिन सड़कों के पक्का होना गांव की तरक्की का सुबूत नहीं थी। गांव में पक्के मकान थे, लेकिन कुछेक ही। गांव के प्रधान का मोबाईल नंबर हमारे पास था। बनारस में ही एक जानकार से मिल गया था। लेकिन लहरतारा के पास ही कटवां गांव.. लहरतारा वहां से तीन किलोमीटर दूर है। हां के निवासियों ने बताया कि प्रधानजी के पास जाएंगे तो वह सच का सामना क्योंकर करवाने लगे?बहरहाल, गांव के प्रायः हरेक घर से खटा-खटाखट की आवाज़ आ रही थी। हथकरघे की..। कबीर जी साकार हो गए। दूर किसी घर में किसी मरदाना आवाज़ ने स्वागत किया... झीनी-झीनी बीनी चदरिया बीनी रे बीनी.. काहे का ताना काहे का भरनी....देखा सफेद दाढी में शख्स। हमें देखते ही राम-राम।
ताज्जुब हुआ। हमने कहा अस्सलामवालेकुम..। उत्तर आया राम-राम। हमारी हैरत पर और परदे डालते हुए उन्होंने कहा हम हिंदुओं और मुसलमानों का फरक नहीं करते। सिर झुक गया। असली हिंदोस्तां यहीं है, न अयोध्या में है,न गोधरा में.. न सांप्रदायिक रंग लिए किसी और जगह।
इसी धंधे में लगे मो. अल हुसैन हमसे मिले। कम होती मज़दूरी ने इन्हें इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो अपनी बेटी को स्कूल भी भेज सकें। आखिर इन्हें पेट और पढाई में से एक ही चीज़ चुननी थी और इन्होंने पेट को तरजीह दी, देनी ही थी। उनकी बेटी पोलियोग्रस्त है.. उनकी शादी की चिंता भी है। हम नीम की घनी छाया में बैठे। नौजवान बुनकर भी कबीर ही गुनगुना रहे थे। एक ने फिल्मी रोमांटिक तान छेड़ी..स्वाति मुस्कुरा उठी...। हमें भी अच्छा लगा। आनंद अपने काम में लगे रहे।
तब तक कोक की बोतल में हैंडपंप का शीतल जल आ गया। कोक की पहुंच यहां तक हो गई है। लेकिन राहत ये कि सिर्फ बोतल था, पानी ऑरिजिनल था। अजब मिठास था पानी में। एक बुजुर्ग प्लेट में दोलमोठ और बिस्कुट ले आए. हमें बहुत शर्म आई.. तकरीबन पूरा गांव शूटिंग देख रहा था, खिड़कियों से झांकती पर्दानशीं महिलाएं.. बकरियों के आगे पीछे खड़े नंग-धडग बच्चे।
गांव में पीने के पानी की समस्या थी। पूरे गांव में एक मात्र हैंड पंप है जो नीम के पेड़ के नीचे है।मंदी के असर से खूबसूरत और दिलकश बनारसी साड़ियों की मांग पर असर पड़ा है। और जाहिर है, बनारस के आसपास के गांव के बुनकर इससे परेशान हैं। बुनकरो की रोजाना दिहाड़ी पहले ६०-७० पुरये थी अब वह ४० रुपये हो गई है। मंहगाई ने कमर पहले से तोड़ दी है। बुनकरो को मलाल है कि उनकी माली हालत पर किसी की नज़र नहीं। बिचौलियों और साहूकारों के कर्ज़ से दबे बुनकर अपनी शिकायत करें भी तो किससे। मंदी में साडियों की मांग में आई कमी ने उनकी हालत सोचनीय बना दी है।
बहरहाल, शूटिंग पूरी होते और बाईट लेते दोपहर बीत गई। हमें फिर बनारस वापस भी जाना था. बल्कि यूं कहें कि मुझे एक और तीर्थ जाना था जहां जाने का सपना संजोये मैं दिल्ली निकला था। जल्ली-जल्दी दालमोठ फांक कर और कबीर के गांव मे ढेर सारा निर्मल जल पीकर मैं वापसी की तैयारियों में लग गया। सारा गांव हमें छोड़ने बाहर तक आ रहा था। आनंद जी ने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी.. खूबसूरत मरुन कलर की साड़ी..
मंजीत ठाकुर, लहरतारा गांव बनारस से
Saturday, July 11, 2009
कबीर के गांव में
अनिंद्यो (हमारे बॉस) ने मेसेज किया, मधुर जलपान में मीठा खाना, और रामनगर तक मुंह अँधेर नाव की सवारी का मजा़ लिजिए। कैमरामैन ने मना कर दिया। मैं अकेला था जिसे रुचि थी। सवेरे उठना मेरे लिए थोड़ा, थोड़ा क्या पूरा नामुमकिन है। लेकिन पता नहीं किस शक्ति ने मुझे जगा दिया। सबों को छोड़कर मैं चल दिया। ड्राइवर मेरे साथ था। लखनऊ वाले थे, उनने एक मुहावरा कहा- जिसका अर्थ है, कि इंसानों के पूर्वज अदरक का स्वाद नहीं जानते। इसके तहकीकात में न जाते हुए मैं रामनगर तक नाव की सवारी करता गया। और उस पल का मजा... मेरे पास शब्द नहीं है।
पूरब से उगता हुआ लाल गोला.. मान्यताओं पर भरोसा करें तो ऐसे ही किसी पल में पवनपुत्र हनुमान ने उसे निगल लेने की हिमाकत की होगी। गंगा का पानी पहले तो ललछौंह हुआ फिर सुनहरे में तब्दील हो गया। पिघले हुए सोने के माफिक..। लगा लावा उमड़ रहा हो..। आसपास तैरती कश्तियां..उस पर नाव की सवारी का मजा़ लेते देशी-विदेशी सैलानी।
बहरहाल, सुबह सवेरे मिष्टान्न का अल्पाहार..(वह मेरे लिए अल्पाहार था, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा) संपन्न होने के बाद जब मैं होटल पहुंचा तो टीम के मेंबरान घोड़े बेचे हुए थे।
उनके नाश्ता वगैरह से फारिग होते साढे नौ बज गए। स्वाति भी पहुंच गई, दीदी ने पूरियां भेजी थीँ। उसे उदरस्थ कर हम काम पर चले। लहरतारा..। कबीर वहीं जन्मे थे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे.. पटना में बलराम तिवारी कबीर के बारे में बताते हुए भावुक हो जाते थे।
''जों हम मरिहें तो राम भी मरिहें...
जों राम न मरिहें तो हम काहे को मरिहें... ''
या फिर,
''मैं तो कूतरा राम का मोतिया मेरा नाम....''
मेरे बचपन में पिताजी एक कबीर का एक पद गाया करते थे,
''झीनी-झीनी बीनी चदरिया बीनी रे ''बीनी,...... कानों में गूंज रहा था।
एक राहगीर से हमने पूछा, लहरतारा किधर है? उसने सादर कहा, साहबजी के गांव? और रास्ता बता दिया.. नौ किलोमीटर पूरब..। एक बेहद आध्यात्मिक-सा अनुभव अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। लगा कि लहरतारा डा रहा हूं, मगहर भी ज़रुर जाऊंगा।
जारी...
भाई सुशांत ने इलाहाबाद पर लिखने को कहा है, अब मैं क्या लिखूं? सारा कुछ तो आपने बयां कर दिया है, अपने पोस्ट में। बेहद शानदार.. मेरे अनुभव भी आपकी ही तरह हैं, सच मानिए.. मेरे दिल की बात उनके पोस्ट में हैं। चलो अपने ब्लॉग पर मैं इलाहाबाद के बारे में कुछ नहीं लिखता.. आगे बनारस के बारे में ही लिख रहा हूं।
Monday, July 6, 2009
मेरा भारतनामा-२ कानपुर में एक दिन

कानपुर में सुबह को उठते-उठते देर हो गई थी। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा था कि कानपुर भारत का मैनचेस्टर है। शायद इसी उत्सुकता की वजह से हमने वहां कि सूती मिलों का जायज़ा लेने का फैसला किया। लेकिन लक्ष्मी रतन कॉटन मिल हो या ऐसी ही दूसरी मिलें, ज्यादातर मिलें बंद पड़ी हैं। हमें बेहद निराशा हुई लेकिन एक स्टोरी मिल गई थी, इसकी खुशी भी थी।
हमने बचपन में लाल इमली का नाम भी बहुत सुना था। लाल इमली नामी ऊनी कपड़ों का ब्रांड था। लाल इमली कारखाना एशिया का सबसे बड़ा ऊन कारखाना था। लेकिन वक्त के साथ इस कारखाने की तकदीर भी बदल गई। ( १९८९ तक सबकुछ ठीक-ठाक था, लेकिन ९० के दशक में कारखाने की सेहत गिरती चली गई। सरकरा ने वक्त-वक्त पर राहत के कुछ पैकेज ज़रुर दिए, लेकिन वह मिल को संभालने के लिए नाकाफी साबित हुए।
लाल इमली के कारखाने की इमारत अगर आप देखें तो ये अपनी भव्यता और इतिहास की दुहाई देता मालूम होता है।
Tuesday, June 30, 2009
लालगढ़ः बोउदी-र होटेल
Monday, June 29, 2009
आज का विचार-२
१. जो पसंद है उसे हासिल करना सीख
२. जो हासिल है, उसे पसंद करना सीख लें.
मंजीत ठाकुर, मेदिनीपुर से दार्शनिक मूड में क्योंकि मूड सही नहीं है।
Wednesday, June 24, 2009
मेरा भारतनामा- दिल्ली से कोलकाता, पहला पड़ाव
देश की धड़कन देखने निकला हूं, कोलकाता की ओर..। सड़क के रास्ते दिल्ली से कोलकाता.....
बॉस के आइडिए ने दिल और दिमाग झंकृत कर दिया मेरा तो। कार्यक्रम है बजट यात्रा । बजट से ऐन पहले देश कीजनता की समस्याओं पर कुछ काम किया जाए। काम न भी हो कम से कम जनता का मिज़ाज तो भांप ही लिया जाए।
मेरा रुट बना, दिल्ली से मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद होते बनारस, सारनाथ, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, होते कुशीनगर से बेतिया, मोतिहारी, मुजफ़्फ़रपुर, पटना, नालंदा, बिहार शरीफ, नवादा, कोडरमा, हज़ारीबाग़, फिर वहां से इसरी-डुमरी-पारसनाथ होते आसनसोल, पानागढ़, वर्धवान, दुर्गापुर, फिर वहां से कोलकाता।
हमारा सफर १५ तारीख को शुरु हुआ। गनीमत ये रही कि एसी गाड़ी मिल गई। साथ में कैमरामैन आनंद प्रकाश और सुनील के साथ साथी रिपोर्टर थी स्वाति बक्षी। स्वाति गरमी से परेशान थी।
सुबह को सफर की शुरुआत हुई तो मजा़ आ रहा था। स्वाति खेतों की कथित हरियाली से खुश थी। पलवल में जाकर सड़क के किनारे चाय पी। स्वाति और आनंद घर का खाना लेकर आए थे। मैंने खूब चकल्लस उडा़या। घर का खाना, आगे नहीं मिलने वाला था।
हालांकि इस बात से मैं जरा भी परेशान नहीं था, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान मैं ट्रक ड्राइवरो वाली जिंदगी जी चुका था। स्वाति अनजान थी कि आगे क्या होने वाला है। मथुरा में लस्सी पीते, आगरा में कुछ खाते हम रास्ते में शूट भी करते जा रहे थे। खेतों में मूंग की फसल प्रौढ़ हो चुकी थी, उनकी फलियों को तोड़ने वाली महिलाओं में लेकिन नौजवान भी थीं, बच्चियां भी,।
वहीं स्वाति ने पहली बार कच्चे मूंग का स्वाद चखा। अपना ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए यह सब पहली बार नहीं था। उसे मैंने खेतों की मेढ़ पर उगे भांग की पत्तियां भी दिखाईँ। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस मारिजुआना की बात इतने अदब से की जाती है , वह दरअसल देसी भांग ही है।
मैंने समझाने की कोशिश की कि देसी चीज़े हीं परदेश आकर बदल जाती हैं। मुलम्मा चढ़ते ही स्वाद बदल जाता है। गांव का कच्चापन शहर आते ही रंग बदल लेता है। वरना मारिजुआना की गोली में क्या दम कि वह गांव की ठंडई का मुकाबला कर ले।
बहरहाल, उसने भांग की कुछ पत्तियों को अपने हैंडबैग में बतौर अमानत छुपा लिया। आनंद ने गुजारिश की कि बिहार या झारखंड में उसे ताड़ी पिलवाऊं। मैंने उसे देशी स्कॉच के बारे में बहुत कुछ बताया था। कहा था कि इसका नशा सूरजमुखी के फूल की तरह दिन चढ़ने के साथ बड़ता है। देह में हवा लगते ही आदमी बहकता है, मानो बसंती हवा हो।
ड्राइवर थोड़े बुजुर्ग थे, लेकिन वह बुजुर्ग भी क्या बुजुर्ग जिसे मेरा साथ मिलते ही जवानी न उबाल मारने लगे। साहब, ऐसी घुट्टी कान में पिलाई कि इनोवा ने ८० छोड़ ११० की रफ्तार पकड़ी। ये रफ्तार जरुरी थी, वरना कानपुर पहुचंते देर हो जाती, या रास्ते में लटक जाते तो सारा शिड्यूल गड़बड़ हो जाता।
तेजी़ के बावजूद कानपुर पहुचंते रात के ११ बज गए। रात में वही रुकना हुआ। होटल था किसी चारखंभा कुआं के पास.. इतनी गहरी नींद सोए कि रात में सपने भी नहीं आए..। क्या ये शुभ संकेत था?
तस्वीरें रोल में हैं, नेगेटिव निकलते ही पोस्ट करुंगा
जारी....
Monday, June 15, 2009
सिनेमा से पहली मुलाकात-2

जब हम थोड़े और बड़े हुए तो उस काले परदे के आगे की दुनिया की खबर लेने की इच्छा बलवती होती गई। तब कर एक और सिनेमाघर शहर में बन गया। सिनेमाघर की पहली फिल्म थी- याराना। सन बयासी का साल था शायद। हम छोटे ही थे, लेकिन भाई के साथ फिल्म देखने के साथ गया। अमिताभ से पहला परिचय याराना के जरिए हुआ।
उस समय तक हमारे क़स्बे में वीडियों का आगाज़ नहीं हुआ था। बड़े भाई आसनसोल से आते तो बताते टीवी और वीडियो के बारे में। हॉल जैसा दिखता है या नहीं?? पता चला बित्ते भर के आदमी दिखते हैं, छोटा सा परदा होता है। निराश हो गया मैं । लेकिन घर पर भी लगा सकते हैं यह अहसास खुश कर गया।
बहरहाल, हमारे शहर में एक राजबाड़ी नाम की जगह है, जहां लड़कों ने आसनसोल से वीडियो लाकर फिल्में दिखाने का फैसला किया था। टिकट था - एक रुपया। औरतो के लिए फिल्म दिखाई जा रही थी-मासूम और एक और फिल्म थी दीवार। मम्मी और उनकी सहेलियां मासूम देखने गईँ। शाम में दीवार दिखाई जानी थी, बाद में जब हम और रतन भैया फिल्म देखकर लौट रहे थे। हम दोनों में विजय बनने के लिए झगड़ा हो गया। वह कहते रहे कि तुम छोटे हो कायदे से रवि तुम बनोगे, लेकिन रवि जैसा ईमानदार बनना मुझे सुहा नहीं रहा था। विजय की आँखों की आग अच्छी लगी और उस दिन के बाद से लगती ही रही।
उस दिन के बाद से फिल्मों का चस्का लग गया। आर्थिक कारणों से अहब मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। वजह-पिताजी का देहांत हो गया। घर में एक किस्म की संजीदगी आ गई थी। मम्मी, मां में बदल गई। उनके सरला, रानू और बाकी के उपन्यास पढ़ना छूट गया। बड़े भैया कमाने पर उतरे, मंझले भाई में पढाई का चस्का लगा। मुझे बेवजह ज्यादा प्यार मिलने लगा। घर के लोग सिनेमा से दूर होते गए। सबका बकाया मैं और बड़े भैया पूरा करने लगे।
सरकारी स्कूल से भाग कर सिनेमा देखने जाने लगा। लेकिन तीन घंटे तक स्कूल और घर से दूर रहने की हिम्मत नहीं थी। उन दिनों -८६ का साल था- मधुपुर के सिनेमाघरों में जबरदस्ती इंटरवल के बाद घुस आने वालों को रोकने के लिए एक नई तरकीब अपनाई गई थी। इंटरवल में बाहर निकलते वक्त गेटकीपर एक ताश के पत्ते का टुकडा़ देता था। अब हमने एक और दोस्त के साथ िस तरकीब का फायदा उठाया। इस तरीके में हम इंटरवल के पहले की फिल्म एक दिन और बाद का हिस्सा दूसरे दिन देख लेते थे।
गिरिडीह में सवेरा सिनेमा हो, या देवघर में भगवान टाकीज, मधुपुर में मधुमिता और सुमेर, आसनसोल में मनोज टाकीज, हर सिनेमाहॉल का पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हमें पहचानने लगा. गेटकीपरों के साथ दोस्ती हो गई। फिल्म देखना एक जुनून बन गया। कई बार हमारे बड़े भाई ने सिनेमाहॉल में ही पकड़ कर दचककर कूटा। लेकिन हम पर असर पड़ा नहीं।
बाद में अपने अग्रीकल्चर कॉलेज के दिनों में या बाद में फिल्में पढाई के तनाव को दूर करने का साधन बन गईं। अमिताभ के तो हम दीवाने थे। शुरु में कोशिश भी की अंग्रेजी के उल्टे सात की तरह पट्टी बढा़ने की , लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। बाद में शाहरुख ने अमिताभ को रिप्लेस करने की तरकीबें लगाईं, तो डीडीएलजे ने बहुत असर छोड़ा था हम पर। नकारात्मक भूमिकाओं को लेकर मै हमेशा से सकारात्मक रहा हूं। ऐसे में बाजीगर और डर वाले शाहरुख को हमने बहुत पसंद किया था। उसके हकलाने की कला, साजन में संजय के बैसाखी लेकर लंगड़ाने की अदा, अजय देवगन की तरह फूल और कांटे वाला सोशल एलियनेशन, .. सब पर हाथ आजमाया।
लेकिन दूरदर्शन की मेहरबानी से फिल्मों से हमारा रिश्ता और मजबूत ही हुआ। दूरदर्सन पर मेरी पहली फिल्म याद नहीं आ रहा साल लेकिन समझौता थी। गाना अब भी याद है समझौता गमो से कर लो..। फिर अमृत मंथन, अवतार, मिर्च-मसाला, पेस्टेंजी, आसमान से गिरा, बेनेगल निहलाणी की फिल्में देखने का शौक चर्राया।
लगा कि मिथुन के हिटलर,जल्लाद, और गोविंदा की कॉमिडी से इतर भी फिल्में हो सकती हैँ। तो हर तरह की फिल्में देखना शुरु से शौक में शामिल रहा। और दूरदर्शन की इसमें महती भूमिका रही। जिसने कला फिल्में देखने की आदत डाल दी. तो हर स्तर की हिंदी अंग्रेजी फिल्में देखते रहे। हां, डीडी की कृपा से ही ऋत्विक घटक और सत्यजित् रे की फिल्मों से परिचय हुआ। तो सिनेमा एक शगल न रह कर ज़रुरत में बदल गया।
बहुत बाद में २००७ में एफटीआईआई में फिल्म अप्रीशिएशन के लिए पहुंचा तो पता चला कि एक पढाई ऐसी भी होती है जिसमे पढाई के दौरान फिल्मे दिखाई जाती हैं। तो पूरे कोर्स को एंजाय किया। फिल्में देखने और फिल्मे पढ़ने की तमीज आई। विश्व सिनेमा से परिचय गाढा हुआ।
गोवा और ओसियान जैसे फिल्मोत्सवों में ईरानी, फ्रेंच और इस्रायली सिनेमा से दोस्ती हुई और सिनेमा का वायरस मुझे नई जिंदगी दे रहा हैं... मैं हर स्तर के फिल्मे जी रहा हूं, और गौरव है मुझे इस बात का कि दुनिया में सिनेमा एक कला और कारोबार के रुप में जिंदा है तो मेरे जैसे दर्शक की वजह से, जो एक ही साथ रेनुवां-फेलेनी और राय-घटक के साथ गोविंदा के सुख, और सांवरिया भी भी झेल सकता है।
Saturday, June 13, 2009
सिनेमा से पहली मुलाकात
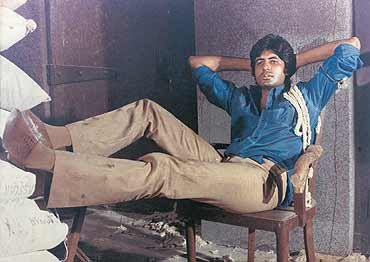
अपने स्कूली दिनों में कायदे से बेवकूफ़ ही था। पढ़ने-लिखने से लेकर सामाजिक गतिविधियों तक में पिछली पांत का खिलाड़ी। क्रिकेट को छोड़ दें, तो बाकी किसी चीज़ में मेरी दिलचस्पी थी ही नहीं। बात तबकी है जब मैं महज सात-आठ साल का रहा होऊंगा।.. मेरे छोटे-से शहर मधुपुर में तब, दो ही सिनेमा हॉल थे, वैसे आज भी वही दो हैं।
लेकिन सिनेमा से पहली मुलाकात, याद नहीं कि कौन सी फिल्म थी वह- मम्मी के साथ हुई थी। मम्मी और कई पड़ोसिनें, मैटिनी शो में फिल्में देखने जाया करतीं। हम इतने छोटे रहे होंगे कि घर पर छोड़ा नहीं जा सकता होगा। तभी हमें मम्मी के साथ लगा दिया जाता होगा। बहनें भी साथ होतीं.. तो सिनेमा के बारे में जो पहली कच्ची याद है वह है हमारे शहर का मधुमिता सिनेमा..।
यह पहले रेलवे का यह गौदाम थी, थोड़ा बहुत नक्शा बदल कर इसे सिनेमा हॉल में तब्दील कर दिया था। ्ब इस हॉल को पुरनका हॉल कहा जाता है। महिलाओं के लिए बैठने का अलग बंदोबस्त था। आगे से काला पर्दा लटका रहता.. जो सिनेमा शुरु होने पर ही हटाया जाता। तो सिनेमा शुरु होने से पहले जो एँबियांस होता वह था औरतों के आपस में लड़ने, कचर-पचर करने, और बच्चों के रोने का समवेत स्वर।
लेडिज़ क्लास की गेटकीपर भी एक औरत ही थीं, मुझे याद है कुछ शशिकलानुमा थी। झगड़ालू, किसी से भी ना दबने वाली..। चूंकि हमारे मुह्ल्ले की औरतें प्रायः फिल्में देखनो को जाती तो सीट ठीक-ठाक मिल जाती। शोहदे भी उस वक्त कम ही हुआ करते होंगे, ( आखिरकार हम तब तक जवान जो नहीं हुए थे) तभी औरतों की भीड़ अच्छी हुआ करती थी।
बहरहाल, फिल्म के दौरान बच्चों की चिल्ल-पों, दूध की मांग, उल्टी और पैखाने के बीच हमारे अंदर सिनेमा के वायरस घर करते गए। हमने मम्मी के साथ जय बाबा अमरनाथ, धर्मकांटा, संपूर्ण रामायण, जय बजरंगबली, मदर इंडिया जैसी फिल्में देखी। रामायण की एक फिल्म में रावण के गरज कर - मैं लंकेश हूं कहने का अंदाज़ मुझे भा गया। और घर में अपने भाईयों और दोस्तों के बीच मैं खुद को लंकेश कहता था।मेरे पुराने दोस्त और रिश्तेदार अब भी लंकेश कहते हैं। वैसे लंकेश का चरित्र अब भी मुझे मोहित करता है, और इसी चरित्र की तरह का दूसरा प्रभावी चरित्र मुझे मोगंबो का लगा। लेकिन तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। और मानने लगा था कि अच्छी नायिकाओं का सात पाने के लिए अच्छा और मासूम दिखने वाला अनिल कपूर या गुस्सैल अमित बनना ज्यादा अहम है।
to be cont...
